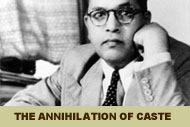♦ शेष नारायण सिंह
महात्मा गांधी की किताब हिंद स्वराज की शताब्दी के वर्ष में कई स्तरों पर उस किताब की चर्चा हो रही है, जो जायज भी है। महात्मा जी की इसी किताब ने सत्याग्रह और अहिंसा को राजनीतिक विजय के एक हथियार के रूप में विकसित करने की प्रेरणा दी और 1920 से 1947 तक की भारत की राजनीतिक यात्रा के पाथेय के रूप में हिंद स्वराज में बताये गये मंत्र अमर हो गये।
दरअसल हिंद स्वराज एक ऐसी किताब है, जिसने भारत के सामाजिक राजनीतिक जीवन को बहुत गहराई तक प्रभावित किया। बीसवीं सदी के उथल पुथल भरे भारत के इतिहास में जिन पांच किताबों का सबसे ज़्यादा योगदान है, हिंद स्वराज का नाम उसमें सर्वोपरि है। इसके अलावा जिन चार किताबों ने भारत के राजनीतिक सामाजिक चिंतन को प्रभावित किया उनके नाम हैं, भीमराव अंबेडकर की
जाति का विनाश मार्क्स और एंगेल्स की
कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ज्योतिराव फुले की
गुलामगिरी और वीडी सावरकर की
हिंदुत्व। अंबेडकर, मार्क्स और सावरकर के बारे में तो उनकी राजनीतिक विचारधारा के उत्तराधिकारियों की वजह से हिंदी क्षेत्रों में जानकारी है। क्योंकि मार्क्स का दर्शन कम्युनिस्ट पार्टी का, सावरकर का दर्शन बीजेपी का और अंबेडकर का दर्शन बहुजन समाज पार्टी का आधार है लेकिन 19 वीं सदी के क्रांतिकारी चितंक और वर्णव्यवस्था को गंभीर चुनौती देने वाले ज्योतिराव फुले के बारे में जानकारी की कमी है। ज्योतिराव गोविंदराव फुले का जन्म पुणे में हुआ था और उनके पिता पेशवा के राज्य में बहुत सम्माननीय व्यक्ति थे। लेकिन ज्योतिराव फुले अलग किस्म के इंसान थे। उन्होंने दलितों के उत्थान के लिए जो काम किया उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। उनका जन्म 1827 में पुणे में हुआ था, माता पिता संपन्न थे लेकिन महात्मा फुले हमेशा ही गरीबों के पक्षधर बने रहे। उनकी महानता के कुछ खास कार्यों का ज़िक्र करना ज़रूरी है।
1848 में शूद्रातिशूद्र लड़कियों के लिए एक स्कूल की स्थापना कर दी थी। आजकल जिन्हें दलित कहा जाता है, महात्मा फुले के लेखन में उन्हें शूद्रातिशूद्र कहा गया है। 1848 में दलित लड़कियों के लिए स्कूल खोलना अपने आप में एक क्रांतिकारी कदम है। क्योंकि इसके 9 साल बाद बंबई विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। उन्होंने 1848 में ही मार्क्स और एंगेल्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किया था। 1848 में यह स्कूल खोलकर महात्मा फुले ने उस वक्त के समाज के ठेकेदारों को नाराज़ कर दिया था। उनके अपने पिता गोविंदराव जी भी उस वक्त के सामंती समाज के बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। दलित लड़कियों के स्कूल के मुद्दे पर बहुत झगड़ा हुआ लेकिन ज्योतिराव फुले ने किसी की न सुनी। नतीजतन उन्हें 1849 में घर से निकाल दिया गया। सामाजिक बहिष्कार का जवाब महात्मा फुले ने 1851 में दो और स्कूल खोलकर दिया। जब 1868 में उनके पिताजी की मृत्यु हो गयी तो उन्होंने अपने परिवार के पीने के पानी वाले तालाब को अछूतों के लिए खोल दिया। 1873 में महात्मा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की और इसी साल उनकी पुस्तक गुलामगिरी का प्रकाशन हुआ। दोनों ही घटनाओं ने पश्चिमी और दक्षिण भारत के भावी इतिहास और चिंतन को बहुत प्रभावित किया।
महात्मा फुले के चिंतन के केंद्र में मुख्य रूप से धर्म और जाति की अवधारणा है। वे कभी भी हिंदू धर्म शब्द का प्रयोग नहीं करते। वे उसे ब्राह्मणवाद के नाम से ही संबोधित करते हैं। उनका विश्वास था कि अपने एकाधिकार को स्थापित किये रहने के उद्देश्य से ही ब्राह्मणों ने श्रुति और स्मृति का आविष्कार किया था। इन्हीं ग्रंथों के जरिये ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था को दैवी रूप देने की कोशिश की। महात्मा फुले ने इस विचारधारा को पूरी तरह ख़ारिज़ कर दिया। फुले को विश्वास था कि ब्राह्मणवाद एक ऐसी धार्मिक व्यवस्था थी जो ब्राह्मणों की प्रभुता की उच्चता को बौद्घिक और तार्किक आधार देने के लिए बनायी गयी थी। उनका हमला ब्राह्मण वर्चस्ववादी दर्शन पर होता था। उनका कहना था कि ब्राह्मणवाद के इतिहास पर गौर करें तो समझ में आ जाएगा कि यह शोषण करने के उद्देश्य से हजारों वर्षों में विकसित की गयी व्यवस्था है। इसमें कुछ भी पवित्र या दैवी नहीं है। न्याय शास्त्र में सत की जानकारी के लिए जिन 16 तरकीबों का वर्णन किया गया है, वितंडा उसमें से एक है। महात्मा फुले ने इसी वितंडा का सहारा लेकर ब्राह्मणवादी वर्चस्व को समाप्त करने की लड़ाई लड़ी। उन्होंने अवतार कल्पना का भी विरोध किया। उन्होंने विष्णु के विभिन्न अवतारों का बहुत ही ज़ोरदार विरोध किया। कई बार उनका विरोध ऐतिहासिक या तार्किक कसौटी पर खरा नहीं उतरता लेकिन उनकी कोशिश थी कि ब्राह्मणवाद ने जो कुछ भी पवित्र या दैवी कह कर प्रचारित कर रखा है उसका विनाश किया जाना चाहिए। उनकी धारणा थी कि उसके बाद ही न्याय पर आधारित व्यवस्था कायम की जा सकेगी। ब्राह्मणवादी धर्म के ईश्वर और आर्यों की उत्पत्ति के बारे में उनके विचार को समझने के लिए ज़रूरी है कि यह ध्यान में रखा जाए कि महात्मा फुले इतिहास नहीं लिख रहे थे। वे सामाजिक न्याय और समरसता के युद्घ की भावी सेनाओं के लिए बीजक लिख रहे थे।
महात्मा फुले ने कर्म विपाक के सिद्घांत को भी ख़ारिज़ कर दिया था, जिसमें जन्म जन्मांतर के पाप पुण्य का हिसाब रखा जाता है। उनका कहना था कि यह सोच जातिव्यवस्था को बढ़ावा देती है इसलिए इसे फौरन ख़ारिज़ किया जाना चाहिए। फुले के लेखन में कहीं भी पुनर्जन्म की बात का खंडन या मंडन नहीं किया गया है। यह अजीब लगता है क्योंकि पुनर्जन्म का आधार तो कर्म विपाक ही है।
महात्मा फुले ने जाति को उत्पादन के एक औज़ार के रूप में इस्तेमाल करने और ब्राह्मणों के आधिपत्य को स्थापित करने की एक विधा के रूप में देखा। उनके हिसाब से जाति भारतीय समाज की बुनियाद का काम भी करती थी और उसके ऊपर बने ढांचे का भी। उन्होंने शूद्रातिशूद्र राजा, बालिराज और विष्णु के वामनावतार के संघर्ष का बार-बार ज़िक्र किया है। ऐसा लगता है कि उनके अंदर यह क्षमता थी कि वह सारे इतिहास की व्याख्या बालि राज-वामन संघर्ष के संदर्भ में कर सकते थे।
स्थापित व्यवस्था के खिलाफ महात्मा फुले के हमले बहुत ही ज़बरदस्त थे। वे एक मिशन को ध्यान में रखकर काम कर रहे थे। उन्होंने इस बात के भी सूत्र दिये, जिसके आधार पर शूद्रातिशूद्रों का अपना धर्म चल सके। वे एक क्रांतिकारी सामाजिक परिवर्तन की बात कर रहे थे। ब्राह्मणवाद के चातुर्वर्ण्य व्यवस्था को उन्होंने ख़ारिज़ किया, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त का, जिसके आधार पर वर्णव्यवस्था की स्थापना हुई थी, को फर्ज़ी बताया और द्वैवर्णिक व्यवस्था की बात की।
महात्मा फुले एक समतामूलक और न्याय पर आधारित समाज की बात कर रहे थे इसलिए उन्होंने अपनी रचनाओं में किसानों और खेतिहर मजदूरों के लिए विस्तृत योजना का उल्लेख किया है। पशुपालन, खेती, सिंचाई व्यवस्था सबके बारे में उन्होंने विस्तार से लिखा है। गरीबों के बच्चों की शिक्षा पर उन्होंने बहुत ज़ोर दिया। उन्होंने आज के 150 साल पहले कृषि शिक्षा के लिए विद्यालयों की स्थापना की बात की। जानकार बताते हैं कि 1875 में पुणे और अहमदनगर जिलों का जो किसानों का आंदोलन था, वह महात्मा फुले की प्रेरणा से ही हुआ था। इस दौर के समाज सुधारकों में किसानों के बारे में विस्तार से सोच-विचार करने का रिवाज़ नहीं था लेकिन महात्मा फुले ने इस सबको अपने आंदोलन का हिस्सा बनाया।
स्त्रियों के बारे में महात्मा फुले के विचार क्रांतिकारी थे। मनु की व्यवस्था में सभी वर्णों की औरतें शूद्र वाली श्रेणी में गिनी गयी थीं। लेकिन फुले ने स्त्री पुरुष को बराबर समझा। उन्होंने औरतों की आर्य भट्ट यानी ब्राह्मणवादी व्याख्या को ग़लत बताया।
फुले ने विवाह प्रथा में बड़े सुधार की बात की। प्रचलित विवाह प्रथा के कर्मकांड में स्त्री को पुरुष के अधीन माना जाता था लेकिन महात्मा फुले का दर्शन हर स्तर पर गैरबराबरी का विरोध करता था। इसीलिए उन्होंने पंडिता रमाबाई के समर्थन में लोगों को लामबंद किया, जब उन्होंने धर्म परिवर्तन किया और ईसाई बन गयीं। वे धर्म परिवर्तन के समर्थक नहीं थे लेकिन महिला द्वारा अपने फ़ैसले खुद लेने के सैद्घांतिक पक्ष का उन्होंने समर्थन किया।
महात्मा फुले की किताब गुलामगिरी बहुत कम पृष्ठों की एक किताब है, लेकिन इसमें बताये गये विचारों के आधार पर पश्चिमी और दक्षिणी भारत में बहुत सारे आंदोलन चले। उत्तर प्रदेश में चल रही दलित अस्मिता की लड़ाई के बहुत सारे सूत्र गुलामगिरी में ढूंढ़े जा सकते है। आधुनिक भारत महात्मा फुले जैसी क्रांतिकारी विचारक का आभारी है।
(शेष नारायण सिंह। मूलतः इतिहास के विद्यार्थी। पत्रकार। प्रिंट, रेडियो और टेलिविज़न में काम किया। 1992 से अब तक तेज़ी से बदल रहे राजनीतिक व्यवहार पर अध्ययन करने के साथ साथ विभिन्न मीडिया संस्थानों में नौकरी की। महात्मा गांधी पर काम किया। अब स्वतंत्र रूप से लिखने-पढ़ने के काम में लगे हैं। उनसे sheshji@gmail.com पर संपर्क किया जा सकता है।)
 दिलीप मंडल
दिलीप मंडल