
Tuesday, December 29, 2009
आरएसएस, अंतरजातीय विवाह और जाति का अंत
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक मोहन भागवत कहते है कि हिंदू समाज को अब मिलकर जाति पर हल्ला बोल देना चाहिए। जाति का विरोध इस समय फैशन में है। हिंदू समाज में जिस भी व्यक्ति को जाति की चोट नहीं झेलनी पड़ती और किसी खास जाति का होने का नुकसान या अपमान नहीं उठाना पड़ता, वो आसानी से कह सकता है कि मैं जाति को नहीं मानता और भारत में जातिवाद खत्म हो रहा है। ऐसे लोग बसों में साथ चलने, रेस्टोरेंट में साथ खाने और साथ नौकरी करने आदि को जाति के अंत के संकेत के रूप में देख रहे हैं। लेकिन मोहन भागवत जब ये कहते हैं कि जाति का अंत होना चाहिए तो इस पूरी चर्चा के मायने बदल जाते हैं।
मोहन भागवत की आगरा में कही गई बातों को अगर मीडिया ने सही रिपोर्ट किया है (ये खबर दर्जनों जगह छपी है और आरएसएस ने इसका खंडन नहीं किया है) तो उन्होंने न सिर्फ ये कहा है कि जाति के बंधनों की वजह से हिंदुत्व का विकास सैकड़ों वर्षों से रुका हुआ है बल्कि मोहन भागवत हिंदुओं के अंतरजातीय विवाह को जातिवाद की समस्या के समाधान के रूप में देख रहे हैं। आरएसएस प्रमुख ने ये दावा भी किया है कि हाल के किसी सर्वे के मुताबिक अंतरजातीय शादियां करने वालों में आरएसएस से जुड़े लोग सबसे आगे हैं। ऐसा सर्वे कहां हुआ है, उसका विधि क्या थी और सैंपल साइज क्या था, इस बारे में जानना रोचक होगा।
आरएसएस आज अगर इस नतीजे पर पहुंचा है कि जातिवाद से हिंदुत्व का नुकसान हुआ है तो ये शुभ है लेकिन साथ ही बेहद आश्चर्यजनक भी है। उससे भी आश्चर्यजनक है आरएसएस द्वारा हिंदुओं के अंतरजातीय विवाह का समर्थन। आरएसएस से जुड़े किसी भी आधिकारिक साहित्य में अंतरजातीय विवाह का समर्थन नहीं मिलता। जातिवाद का विरोध करना एक बात है। काफी लोग ऐसा जबानी विरोध करते हैं। घनघोर जातिवादी लोग भी जाति के खिलाफ बोलते रहते हैं। लेकिन इस समय आरएसएस का जाति व्यवस्था की जड़ों पर हमला करना और रक्त शुद्धता की अवधारणा का खंडन करना बेहद महत्वपूर्ण है। ये मानने का कोई कारण नहीं है कि आरएसएस को ये मालूम नहीं है कि इसका क्या मतलब है। जाति व्यवस्था को विरोध करना दरअसल सनातम धर्म के मूल का खंडन करना है। हम सब जानते हैं कि कोई भी हिंदू सिर्फ हिंदू नहीं हो सकता। उसे वर्णव्यवस्था की सीढ़ी में कहीं न कहीं होना ही होगा। किसी जाति का होना होगा। उस जाति के ऊपर या नीचे या ऊपर और नीचे भी किसी न किसी जाति को होना होगा। ऋग्वेद से लेकर श्रीमद्भगवतगीता की अलग अलग व्याख्याएं हिंदू धर्म के इस अविकल सत्य को स्थापित करती हैं। इस बिंदु पर हिंदू धर्म के टीकाकारों में कोई मतभेद नहीं है।
यही वजह है कि किसी हिंदू का अन्य धर्म में जाना यानी धर्मांतरण संभव है, लेकिन किसी और धर्म के व्यक्ति का हिंदू धर्म में धर्मांतरण मुमकिन नहीं है क्योंकि उसे किस जाति में रखा जाए, इसकी समस्या होती है। किसी जाति का हुए बिना रोटी का संबंध तो फिर भी कायम हो सकता है लेकिन बेटी यानी शादी का संबंध कैसे कायम हो सकता है? धर्मांतरण के नाम पर हिंदुत्ववादी संगठन शुद्धिकरण करके कुछ लोगों की हिंदू धर्म में वापसी करा पाते हैं क्योंकि शुद्धिकरण करते समय ये पता होता है कि वो व्यक्ति या समूह पहले किस हिंदू जाति में था। मिसाल के तौर पर अगर किसी दलित ने या उसके पूर्वज ने इस्लाम या कोई और धर्म अपना लिया था, तो शुद्धिकरण कर उसे फिर से दलित जाति का हिस्सा बनाया जा सकता है। लेकिन अगर किसी अन्य देश के ईसाई या मुसलमान या यहूदी व्यक्ति का हिंदू बन पाना संभव नहीं है।
ऐसी कठोर जाति व्यवस्था में बंटे समाज के लिए अगर मोहन भागवत अंतरजातीय विवाह का मंत्र दे रहे हैं तो इसका स्वागत होना चाहिए। हिंदुओं ने जाति व्यवस्था की वजह से काफी तकलीफें सही हैं और देश के विकास में ये एक बड़ी बाधा रही है। मैकाले द्वारा अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिए जाने तक देश के बहुसंख्यक लोगों के लिए शिक्षा के दरवाजे बंद थे क्योंकि गुरुकुलों में सभी जाति के बच्चों का स्वागत नहीं होता था। अभी भी खास जाति के बच्चों के लिए खासकर गांवों में शिक्षा प्राप्त करना आसान नहीं हैं। साथ ही उत्पादन कार्यों में जुटी जातियों को ज्ञान-विज्ञान की शिक्षा से दूर रखे जाने के कारण भारत में विज्ञान की जीवंत परंपरा बन ही नहीं पाई। ज्ञान का अगर कर्म से संबंध न हो तो ज्ञान का विकास नहीं होता है। यूरोप में वर्कशॉप से निकला अनुभव शिक्षा केंद्रों तक पहुंचा और शिक्षा केंद्रों के ज्ञान की परीक्षा कार्यशालाओं में हुई। भारत में जाति की जकड़बंदी के कारण ये मुमकिन ही नहीं था। ऊंची मानी गई जातियों के लिए मरे हुए को छुने पर धार्मिक निषेध के कारण यहां चिकित्साशास्त्र में शल्य क्रिया की विधा का विकास नहीं हो पाया! ऐसी कई समस्याएं भारत में ज्ञान के विकास में बाधक रही हैं।
ऐसी ही समस्याओं की विरासत हम आज भी ढो रहे हैं। विदेशी हमलावरों के लिए हम हमेशा आसान शिकार रहे क्योंकि चंद जातियों के अलावा बाकी विशाल आबादी के लिए अस्त्र शस्त्र के संधान की तो बात छोड़िए, उन्हें छूने पर भी पाबंदी थी। फुले और आंबेडकर की परंपरा ने इन समस्याओं को काफी पहले चिन्हित कर लिया था। अब अगर आरएसएस भी इसी वैचारिक रास्ते पर चलता है तो इससे बेहतर क्या हो सकता है? लेकिन ये रास्ता आरएसएस के लिए आसान नहीं होगा। संघ का मूल जनाधार हिंदू धर्म में इतने बड़े बदलाव के लिए अभी शायद ही तैयार है। कई लोगों को ये लग सकता है कि अंतरजातीय विवाह से जाति टूटेगी और बड़ी संख्या में जाति से बाहर शादियां होने लगीं, तो जाति और प्रकारांतर में हिंदू धर्म के अस्तित्व पर ही सवाल जरूर खड़ा हो जाएगा।
ये सच है कि शहरीकरण और महिलाओं की शिक्षा और नौकरियों में बढ़ती भागीदारी के कारण अंतरजातीय शादियों को काफी बल मिला है। खासकर शहरों और महानगरों में लोग अब अंतरजातीय शादियों पर पहले की तरह नहीं चौंकते। लेकिन समाज की मुख्यधारा में इसकी मान्यता स्थापित होने में समय लगेगा। साथ ही अंतरजातीय शादियों में भी इस बात का कई बार ध्यान रखा जाता है कि वर्णों की क्रमव्यवस्था यानी हायरार्की में ज्यादा दूरी न हो। इसलिए ब्राह्मण और कायस्थ की शादियां तो फिर भी होती दिखती हैं, दलित वर और ब्राह्मण वधु जैसे जोड़े अपेक्षाकृत कम बन रहे हैं। यानी अंतरजातीय विवाहों में भी जाति का ख्याल कई बार रखा जाता है। वैसे मुंबई के दादर में हुए एक बहुचर्चित शोध (शोधकर्ता : केविन मुंशी और मार्क रोजेनविग) से ये स्थापित हुआ कि अंग्रेजी शिक्षा और अंतरजातीय विवाह का भी रिश्ता है। इस शोध से पता चला कि जिनकी शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से हुई उनमें से 31.6% ने जाति से बाहर शादी की जबकि मराठी माध्यम में शिक्षा प्राप्त करने वालों में अंतरजातीय विवाह का प्रतिशत 10% से भी कम था।
ऐसे में क्या ये माना जाए कि हिंदुत्ववादी संगठन भी समय की बदलती चाल को भांप रहे हैं। उनका जिस शहरी मध्यवर्ग में आधार है, उनके बीच शिक्षा की बदलती प्राथमिकताओं का असर, मुमकिन है कि, ऐसे संगठनों की विचारधारा पर भी पड़ रहा है। अगर सचमुच ऐसा हो रहा है तो ये फुले-आंबेडकर विचारधारा की जीत का जश्न मनाने का समय है। उम्मीद की जानी चाहिए कि आरएसएस अपने प्रमुख के इस विचार पर कायम रहेगा और हिंदू समाज मोहन भागवत के इन विचारों का समर्थन करेगा। हिंदू समाज में व्यापक स्वीकार्यता के बावजूद महात्मा गांधी भी कभी जाति व्यवस्था के अंत की बात नहीं कर पाए। अब अगर आरएसएस हिंदू धर्म की इस कुरीति को खत्म करने के लिए अभियान चलाता है तो ये न सिर्फ हिंदू धर्म और उसके मतावलंबियों के लिए बल्कि पूरे देश के लिए शुभ होगा। ऐसे अभियान की कमान अभी तक समाज में नीचे से हुई है। आरएसएस की पहल की वजह से अब इस अभियान को एक नई दिशा मिल सकती है। ऐसा कामना की जानी चाहिए कि आरएसएस इस अभियान के लिए साहस जुटा पाएगा और 21वीं सदी में ये संगठन अपने लिए एक नया रास्ता चुन पाएगा।
हालांकि इस पहल का स्वागत करते समय एक सावधानी बरतने की भी जरूरत है। जाति के अंत की बात हाल के वर्षों में सबसे ज्यादा उन लोगों ने की है, जो आरक्षण की संवैधानिक व्यवस्था का अंत देखना चाहते हैं। आरक्षण और जाति के आधार पर दूसरे विशेष अधिकारों के विरोधियों की तरफ से ये तर्क बार बार आता है कि समाज में जातपात अब है कहां। सभी तो बराबर हैं। इसलिए अब मेरिट को ही शिक्षा और नौकरियों का एकमात्र आधार माना जाए। इस बात का ध्यान रखना होगा कि जाति विरोध और जाति के अंत की आरएसएस की कामना का निहितार्थ कहीं ऐसा न हो। जब तक जाति है, और जाति के आधार पर अवसरों में भेदभाव है, तब तक जाति के आधार पर शासन की ओर से विशेष व्यवस्था और सुविधा की जरूरत होगी। इसलिए लोकसभा और विधानसभाओं के अलावा बाकी और किसी भी तरह के आरक्षण और जाति के आधार पर विशेष सुविधाओं की व्यवस्था के साथ समय की सीमा नहीं जोड़ी गई है। जब देश में बड़ी संख्या में अंतरजातीय शादियां होने लगेंगी और जाति के आधार पर भेदभाव का अंत हो जाएगा, तब जाति का अस्तित्व नहीं रहेगा और तब आरक्षण न जरूरत होगी न ही कोई इसकी मांग करेगा।
बहरहाल इस समय हिंदू धर्म के तमाम हितरक्षकों को मोहन भागवत के सुझावों और तर्कों पर विचार करना चाहिए। अगर
मोहन भागवत ऐसा कह रहे हैं तो लगता है कि जातिरहित समाज बनाने का समय सचमुच आ गया है!
(यह लेख जनसत्ता के संपादकीय पेज पर छपा है)
Tuesday, December 1, 2009
The Sweetest Little Magenta Flower Girl
Hey Guys,
I thought I must share this exqusite experience I had this morning while returning from my morning walk, I came across this little girl standing by a flower plant outside what could have been her house. She might not have been more than four mind you.
 Like I usually do when I see little kids, I tried to catch her eye and smile and say hello. Guess what ? This benevolent little girl beat me to it! Even before I could smile nd say hello...this little girl plucked a magenta flower,reached out with her tiny hand and gave me the flower with a most beautiful and radiant smile on her face.
Like I usually do when I see little kids, I tried to catch her eye and smile and say hello. Guess what ? This benevolent little girl beat me to it! Even before I could smile nd say hello...this little girl plucked a magenta flower,reached out with her tiny hand and gave me the flower with a most beautiful and radiant smile on her face. I was not expecting something this exquisite to happen to me so i took an extra split second to take in the situation. My heart just melted at this exquisite gesture this little girl made to me. I took the flower with my eyes almost misting and hugged the sweetest little girl in the whole world. I was amazed at her incredible generosity of spirit at age four !!! I instantly fell in love with her.
This incident whose fragrance will not leave me till I die made me think...
What made a little girl reach out and give a flower to a veritable stranger?
Is it due to an innate fearlessness born out of innate love and trust ?
I am known amongst my friends as a very very freindly person but the sweet little flower girl made me realie that I am freindly only with firends or acquaintances!
I am wary of strangers and very suspicious of approaching strangers.
I wondered ....have we forgotten to trust? have we forgotten to reach out and be nice? have we forgetten to make a sweet gesture without expecting anything in return? have we forgotten to smile or be nice to strangers because we fear the consequences which are largely imaginary in nature? would the world be a better place if we exchanged smiles with strangers?
The sweetest little magenta flower girl taught me that if we make a sincere and a sweet gesture out of complete trust and generosity of spirit, then our gesture might almost always be reciprocated.
Thursday, November 26, 2009
क्या फर्क है प्रिंट और वेब पत्रकारिता ?
 दिलीप मंडल
दिलीप मंडलSunday, November 22, 2009
डॉ. अंबेडकर नहीं पढ़ पाए थे जो भाषण, क्या वही है भारत की मुक्ति का मार्ग?
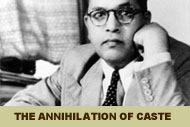

Thursday, November 19, 2009
मेरिट में आगे, जिंदगी में पीछे!

Tuesday, November 17, 2009
रिजर्वेशन: उम्र में छूट किसे चाहिए?

Tuesday, November 3, 2009
गुलामगिरी: एक बेहद जरूरी किताब
महात्मा गांधी की किताब हिंद स्वराज की शताब्दी के वर्ष में कई स्तरों पर उस किताब की चर्चा हो रही है, जो जायज भी है। महात्मा जी की इसी किताब ने सत्याग्रह और अहिंसा को राजनीतिक विजय के एक हथियार के रूप में विकसित करने की प्रेरणा दी और 1920 से 1947 तक की भारत की राजनीतिक यात्रा के पाथेय के रूप में हिंद स्वराज में बताये गये मंत्र अमर हो गये।
दरअसल हिंद स्वराज एक ऐसी किताब है, जिसने भारत के सामाजिक राजनीतिक जीवन को बहुत गहराई तक प्रभावित किया। बीसवीं सदी के उथल पुथल भरे भारत के इतिहास में जिन पांच किताबों का सबसे ज़्यादा योगदान है, हिंद स्वराज का नाम उसमें सर्वोपरि है। इसके अलावा जिन चार किताबों ने भारत के राजनीतिक सामाजिक चिंतन को प्रभावित किया उनके नाम हैं, भीमराव अंबेडकर की जाति का विनाश मार्क्स और एंगेल्स की कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ज्योतिराव फुले की गुलामगिरी और वीडी सावरकर की हिंदुत्व। अंबेडकर, मार्क्स और सावरकर के बारे में तो उनकी राजनीतिक विचारधारा के उत्तराधिकारियों की वजह से हिंदी क्षेत्रों में जानकारी है। क्योंकि मार्क्स का दर्शन कम्युनिस्ट पार्टी का, सावरकर का दर्शन बीजेपी का और अंबेडकर का दर्शन बहुजन समाज पार्टी का आधार है लेकिन 19 वीं सदी के क्रांतिकारी चितंक और वर्णव्यवस्था को गंभीर चुनौती देने वाले ज्योतिराव फुले के बारे में जानकारी की कमी है। ज्योतिराव गोविंदराव फुले का जन्म पुणे में हुआ था और उनके पिता पेशवा के राज्य में बहुत सम्माननीय व्यक्ति थे। लेकिन ज्योतिराव फुले अलग किस्म के इंसान थे। उन्होंने दलितों के उत्थान के लिए जो काम किया उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। उनका जन्म 1827 में पुणे में हुआ था, माता पिता संपन्न थे लेकिन महात्मा फुले हमेशा ही गरीबों के पक्षधर बने रहे। उनकी महानता के कुछ खास कार्यों का ज़िक्र करना ज़रूरी है।
1848 में शूद्रातिशूद्र लड़कियों के लिए एक स्कूल की स्थापना कर दी थी। आजकल जिन्हें दलित कहा जाता है, महात्मा फुले के लेखन में उन्हें शूद्रातिशूद्र कहा गया है। 1848 में दलित लड़कियों के लिए स्कूल खोलना अपने आप में एक क्रांतिकारी कदम है। क्योंकि इसके 9 साल बाद बंबई विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। उन्होंने 1848 में ही मार्क्स और एंगेल्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किया था। 1848 में यह स्कूल खोलकर महात्मा फुले ने उस वक्त के समाज के ठेकेदारों को नाराज़ कर दिया था। उनके अपने पिता गोविंदराव जी भी उस वक्त के सामंती समाज के बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। दलित लड़कियों के स्कूल के मुद्दे पर बहुत झगड़ा हुआ लेकिन ज्योतिराव फुले ने किसी की न सुनी। नतीजतन उन्हें 1849 में घर से निकाल दिया गया। सामाजिक बहिष्कार का जवाब महात्मा फुले ने 1851 में दो और स्कूल खोलकर दिया। जब 1868 में उनके पिताजी की मृत्यु हो गयी तो उन्होंने अपने परिवार के पीने के पानी वाले तालाब को अछूतों के लिए खोल दिया। 1873 में महात्मा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की और इसी साल उनकी पुस्तक गुलामगिरी का प्रकाशन हुआ। दोनों ही घटनाओं ने पश्चिमी और दक्षिण भारत के भावी इतिहास और चिंतन को बहुत प्रभावित किया।
महात्मा फुले के चिंतन के केंद्र में मुख्य रूप से धर्म और जाति की अवधारणा है। वे कभी भी हिंदू धर्म शब्द का प्रयोग नहीं करते। वे उसे ब्राह्मणवाद के नाम से ही संबोधित करते हैं। उनका विश्वास था कि अपने एकाधिकार को स्थापित किये रहने के उद्देश्य से ही ब्राह्मणों ने श्रुति और स्मृति का आविष्कार किया था। इन्हीं ग्रंथों के जरिये ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था को दैवी रूप देने की कोशिश की। महात्मा फुले ने इस विचारधारा को पूरी तरह ख़ारिज़ कर दिया। फुले को विश्वास था कि ब्राह्मणवाद एक ऐसी धार्मिक व्यवस्था थी जो ब्राह्मणों की प्रभुता की उच्चता को बौद्घिक और तार्किक आधार देने के लिए बनायी गयी थी। उनका हमला ब्राह्मण वर्चस्ववादी दर्शन पर होता था। उनका कहना था कि ब्राह्मणवाद के इतिहास पर गौर करें तो समझ में आ जाएगा कि यह शोषण करने के उद्देश्य से हजारों वर्षों में विकसित की गयी व्यवस्था है। इसमें कुछ भी पवित्र या दैवी नहीं है। न्याय शास्त्र में सत की जानकारी के लिए जिन 16 तरकीबों का वर्णन किया गया है, वितंडा उसमें से एक है। महात्मा फुले ने इसी वितंडा का सहारा लेकर ब्राह्मणवादी वर्चस्व को समाप्त करने की लड़ाई लड़ी। उन्होंने अवतार कल्पना का भी विरोध किया। उन्होंने विष्णु के विभिन्न अवतारों का बहुत ही ज़ोरदार विरोध किया। कई बार उनका विरोध ऐतिहासिक या तार्किक कसौटी पर खरा नहीं उतरता लेकिन उनकी कोशिश थी कि ब्राह्मणवाद ने जो कुछ भी पवित्र या दैवी कह कर प्रचारित कर रखा है उसका विनाश किया जाना चाहिए। उनकी धारणा थी कि उसके बाद ही न्याय पर आधारित व्यवस्था कायम की जा सकेगी। ब्राह्मणवादी धर्म के ईश्वर और आर्यों की उत्पत्ति के बारे में उनके विचार को समझने के लिए ज़रूरी है कि यह ध्यान में रखा जाए कि महात्मा फुले इतिहास नहीं लिख रहे थे। वे सामाजिक न्याय और समरसता के युद्घ की भावी सेनाओं के लिए बीजक लिख रहे थे।
महात्मा फुले ने कर्म विपाक के सिद्घांत को भी ख़ारिज़ कर दिया था, जिसमें जन्म जन्मांतर के पाप पुण्य का हिसाब रखा जाता है। उनका कहना था कि यह सोच जातिव्यवस्था को बढ़ावा देती है इसलिए इसे फौरन ख़ारिज़ किया जाना चाहिए। फुले के लेखन में कहीं भी पुनर्जन्म की बात का खंडन या मंडन नहीं किया गया है। यह अजीब लगता है क्योंकि पुनर्जन्म का आधार तो कर्म विपाक ही है।
महात्मा फुले ने जाति को उत्पादन के एक औज़ार के रूप में इस्तेमाल करने और ब्राह्मणों के आधिपत्य को स्थापित करने की एक विधा के रूप में देखा। उनके हिसाब से जाति भारतीय समाज की बुनियाद का काम भी करती थी और उसके ऊपर बने ढांचे का भी। उन्होंने शूद्रातिशूद्र राजा, बालिराज और विष्णु के वामनावतार के संघर्ष का बार-बार ज़िक्र किया है। ऐसा लगता है कि उनके अंदर यह क्षमता थी कि वह सारे इतिहास की व्याख्या बालि राज-वामन संघर्ष के संदर्भ में कर सकते थे।
स्थापित व्यवस्था के खिलाफ महात्मा फुले के हमले बहुत ही ज़बरदस्त थे। वे एक मिशन को ध्यान में रखकर काम कर रहे थे। उन्होंने इस बात के भी सूत्र दिये, जिसके आधार पर शूद्रातिशूद्रों का अपना धर्म चल सके। वे एक क्रांतिकारी सामाजिक परिवर्तन की बात कर रहे थे। ब्राह्मणवाद के चातुर्वर्ण्य व्यवस्था को उन्होंने ख़ारिज़ किया, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त का, जिसके आधार पर वर्णव्यवस्था की स्थापना हुई थी, को फर्ज़ी बताया और द्वैवर्णिक व्यवस्था की बात की।
महात्मा फुले एक समतामूलक और न्याय पर आधारित समाज की बात कर रहे थे इसलिए उन्होंने अपनी रचनाओं में किसानों और खेतिहर मजदूरों के लिए विस्तृत योजना का उल्लेख किया है। पशुपालन, खेती, सिंचाई व्यवस्था सबके बारे में उन्होंने विस्तार से लिखा है। गरीबों के बच्चों की शिक्षा पर उन्होंने बहुत ज़ोर दिया। उन्होंने आज के 150 साल पहले कृषि शिक्षा के लिए विद्यालयों की स्थापना की बात की। जानकार बताते हैं कि 1875 में पुणे और अहमदनगर जिलों का जो किसानों का आंदोलन था, वह महात्मा फुले की प्रेरणा से ही हुआ था। इस दौर के समाज सुधारकों में किसानों के बारे में विस्तार से सोच-विचार करने का रिवाज़ नहीं था लेकिन महात्मा फुले ने इस सबको अपने आंदोलन का हिस्सा बनाया।
स्त्रियों के बारे में महात्मा फुले के विचार क्रांतिकारी थे। मनु की व्यवस्था में सभी वर्णों की औरतें शूद्र वाली श्रेणी में गिनी गयी थीं। लेकिन फुले ने स्त्री पुरुष को बराबर समझा। उन्होंने औरतों की आर्य भट्ट यानी ब्राह्मणवादी व्याख्या को ग़लत बताया।
फुले ने विवाह प्रथा में बड़े सुधार की बात की। प्रचलित विवाह प्रथा के कर्मकांड में स्त्री को पुरुष के अधीन माना जाता था लेकिन महात्मा फुले का दर्शन हर स्तर पर गैरबराबरी का विरोध करता था। इसीलिए उन्होंने पंडिता रमाबाई के समर्थन में लोगों को लामबंद किया, जब उन्होंने धर्म परिवर्तन किया और ईसाई बन गयीं। वे धर्म परिवर्तन के समर्थक नहीं थे लेकिन महिला द्वारा अपने फ़ैसले खुद लेने के सैद्घांतिक पक्ष का उन्होंने समर्थन किया।
महात्मा फुले की किताब गुलामगिरी बहुत कम पृष्ठों की एक किताब है, लेकिन इसमें बताये गये विचारों के आधार पर पश्चिमी और दक्षिणी भारत में बहुत सारे आंदोलन चले। उत्तर प्रदेश में चल रही दलित अस्मिता की लड़ाई के बहुत सारे सूत्र गुलामगिरी में ढूंढ़े जा सकते है। आधुनिक भारत महात्मा फुले जैसी क्रांतिकारी विचारक का आभारी है।
(शेष नारायण सिंह। मूलतः इतिहास के विद्यार्थी। पत्रकार। प्रिंट, रेडियो और टेलिविज़न में काम किया। 1992 से अब तक तेज़ी से बदल रहे राजनीतिक व्यवहार पर अध्ययन करने के साथ साथ विभिन्न मीडिया संस्थानों में नौकरी की। महात्मा गांधी पर काम किया। अब स्वतंत्र रूप से लिखने-पढ़ने के काम में लगे हैं। उनसे sheshji@gmail.com पर संपर्क किया जा सकता है।)
Friday, October 2, 2009
पत्रकारों के पेट तक पहुँचती है लालगढ़ पुलिस की लात?
कोलकाता की पत्रकार बिरादरी उबल रही है, पर दिल्ली में चुप्पी छाई है। एकाध अनुरंजन झा (भड़ास4मीडिया) और अविनाश (मोहल्ला लाइव) को छोड़ दें तो ब्लॉगों पर भी यह सवाल लोगों को मथता नजर नहीं आ रहा। उल्टे यह सवाल उछल रहा है कि जब पत्रकार पुलिस के वेश में या किसी और वेश में खबरें निकाल सकते हैं तो पुलिसवाले पत्रकार का वेश धर कर किसी नक्सली को क्यो नहीं पकड़ सकते?
पहली बात तो यह कि हम किसी पत्रकार, डॉक्टर, गुंडा, आतंकी या नक्सली के आचरण की तुलना पुलिस कार्रवाई से नहीं कर सकते। किसी गुंडे की गोली से एक व्यक्ति का मरना और पुलिस की गोली से मरना - एक जैसी बात नहीं है। पुलिस मौजूदा शासन व्यवस्था का सबसे संगठित हिस्सा है। यही वह ताकत है जिसके जरिए मौजूदा शासन व्यवस्था संचालित होती है।
कहा जा सकता है कि पुलिस वाले भी इंसान होते हैं और उन पर भी काम का वैसा ही बोझ होता है जैसा पत्रकारों पर या किसी भी अन्य पेशे के लोगों पर होता है। बात सही है, लेकिन इसी वजह से यह और भी जरूरी हो जाता है कि शासन व्यवस्था के अन्य संबद्ध हिस्से पुलिस पर अंकुश बनाए रखें। क्योंकि काम के बोझ तले पुलिस में यह स्वाभाविक रुझान होता है कि वह अन्य हिस्सों को अपनी जरूरत के मुताबिक निर्देशित करने की कोशिश करे।
कुछ दिनों पहले नक्सलियों के ही मसले पर इससे मिलती-जुलती सी बहस आंध्र प्रदेश में भी उठी थी। तब आंध्र पुलिस ने पत्रकारों को सलाह दी थी कि वे नक्सली नेताओं से इंटरव्यू न लें, बल्कि अगर उनके पास नक्सली नेताओं के बारे में कोई सूचना हो तो वे पुलिस को दें।
आध्र के पत्रकारों ने इस सलाह पर कड़ा एतराज जाहिर करते हुए कहा था कि हम पुलिस के इन्फोर्मेर नही हैं। पत्रकार का काम पुलिस को नही बल्कि जनता को इन्फोर्म करना होता है। इसीलिये बेहतर यही होगा की पुलिस नक्सलियों को पकड़ने का अपना काम करे और पत्रकारों को अपना काम करने दे।
यही वह बिन्दु है जो पत्रकारों को पुलिस से बुनियादी तौर पर अलग करता है। पुलिस इस तंत्र का एक हिस्सा है जिसका काम इस व्यवस्था को बनाए रखने में मदद करना है। वह सरकार के अधीन होती है, सरकार से ताकत लेती है। इसके विपरीत पत्रकार जनता से ताकत लेते हैं। लोकतंत्र में संप्रभुता जनता में निहित होती है और पत्रकार सीधे जनता को रिपोर्ट करते हैं। इसीलिये सरकार की नाराजगी से उनकी सेहत पर ख़ास फर्क नही पङता।
अरुण शौरी जैसे पत्रकार अगर प्रधान मंत्री की नाराजगी मोल लेते हुए भी शान से पत्रकारिता करते रहे तो उसका कारण यही है की जनता ने उनको मान्यता दी और तत्कालीन सरकार की मर्जी के ख़िलाफ़ दी।
यही बात मौजूदा विवाद पर भी लागू होती है।
सवाल यह नही है कि छत्रधर महतो कितने अच्छे या बुरे हैं और उन्हें पुलिस को पकड़ना चाहिए या नही। उस बारे में फ़ैसला करना अदालत का काम है। यहाँ सवाल यह है कि छत्रधर महतो या उन जैसे लोगो का जो भी कहना है वह सही है या ग़लत इसका अन्तिम फ़ैसला कौन करेगा? ख़ास कर ऐसे विचारधारात्मक मसलों का अन्तिम फ़ैसला सरकार या सरकारी तंत्र के विवेक पर नही छोड़ा जा सकता। लोकतंत्र में, आपको अच्छा लगे या बुरा, पर इसका अन्तिम फ़ैसला जनता के ही पास होता है। वह मौजूदा सरकार ही नही संविधान तक के भविष्य पर विचार करके फैसला कर सकती है।
लेकिन जब तक जनता ऐसा फ़ैसला नही करती तब तक जनता के नाम पर अराजकता फैलाने की भी छूट किसी को नही दी जा सकती। इसीलिये यह व्यवस्था की गयी है कि पुलिस समेत शासन के तमाम अंग अपना काम करते रहें और पत्रकार भी इन तमाम चीजो के बारे में जनता को रिपोर्ट करते रहें।
समस्या तब पैदा होती है जब शासन या इसका कोई अंग (जैसे पुलिस) पत्रकारों को स्वतंत्र तरीके से अपना काम करने से रोकने की कोशिश करता है या अपनी वजहों से इसमे बाधा खड़ी कर देता है।
छत्रधर महतो काण्ड इसी का उदाहरण है जिसमे पुलिस ने पत्रकार के वेश में छत्रधर महतो से संपर्क किया और उसे गिरफ्तार कर लिया। हैरत की बात यह है कि पश्चिम बंगाल के अधिकारी यह मानते हुए भी कि इससे पत्रकारों का काम मुश्किल हुआ है, इसे हंसी में टाल रहे हैं। एक बड़े अधिकारी ने चलताऊ ढंग से पत्रकारों को यह नसीहत दी कि कुछ दिनों तक आप फ़ोन पर बात करके काम चला लें, बाद में जब यह मसला हल हो जाएगा तब फ़िर से इंटरव्यू लेना शुरू कर दीजियेगा।
जब राज्य शासन के सर्वोच्च स्तर पर बैठे अफसर ऐसे मामलो में इतने चलताऊ कमेन्ट कर सकते हैं तो निचले स्तर पर पुलिस अफसरों से भला संवेदनशीलता की उम्मीद कैसे की जा सकती है?
मगर शासन और पुलिस की बात भी बाद में आती है। फिलहाल (कम से कम दिल्ली में) तो हम पत्रकारों को ही यह बात ठीक से समझनी होगी कि यह किसी ख़ास विचारधारा का सवाल नहीं है। यह मामला पत्रकारिता का है, इस बात का है कि पत्रकारों के स्वतंत्र रूप से काम करने की गुंजाइश बनी रहेगी या नही। इसीलए चुप्पी घातक हो सकती है।
Tuesday, September 1, 2009
वक्त बदल गया है, आप भी बदलिए!
मेरे करीबी रिश्तेदारों में कई जातियों के लोग हैं। ब्राह्मण से लेकर कायस्थ और नायर से लेकर दलित तक। ये सभी सभी परिवार प्रेम से रह रहे हैं। आपके परिवारों में भी लोगों ने प्रेम किया होगा और कई ने जाति से बाहर शादियां भी की होंगी। अब आप जाति पर अपने शर्मसार करने वाले विचारों को अपने रिश्तेदारों पर लागू करके देखिए और हिसाब लगाइए कि कौन सी बच्ची या बच्चा कवि बनेगा और कौन कहानीकार और कौन आत्मकथा बेहतर लिखेगा। या हिसाब लगाइए इस बात का कि कौन बैटिंग करेगा और कौन बॉलिंग और कौन टिक कर खेलेगा और कौन टिक कर नहीं खेलेगा या फिर कौन बेहतर नेतृत्व क्षमता दिखाएगा और कौन नहीं दिखाएगा। आपको अपने ही विचारों से शायद नफरत होने लगे और आप अपने बच्चों और पोते-पोतियों से माफी मांगने के अलावा कुछ और नहीं कर पाएं। बड़े लोग जब इस तरह अश्लील और समाज में नफरत फैलाने वाली बातें करने लगें, तो हमारा सिर शर्म से झुक जाता है।
मैं ये सोचने की कोशिश कर रहा हूं कि ये दोनों बुज़ुर्ग बीमार क्यों हैं। इसका एक कारण तो मुझे समझ में आ रहा है। इन्हें दुनिया की शायद खबर ही नहीं है। प्रभाष जोशी इंटरनेट नहीं देखते। वो ऑर्कुट पर नहीं हैं। वो फेसबुक में भी नहीं हैं। मुझे नहीं मालूम कि उनके पास ई-मेल आईडी है या नहीं। कुछ समय पहले तक उनके पास मोबाइल फोन भी नहीं था। एसएमएस पता नहीं वो करते हैं या नहीं। वो ट्विटर पर ट्विट भी नहीं करते। उनका कोई ब्लॉग भी नहीं है। राजेंद्र यादव का भी कमोबेश यही हाल है। वैसे तो इस गरीब देश के ज्यादातर लोगों की प्रोफाइल नेटवर्किंग साइट पर नहीं हैं, वो ईमेल भी नहीं करते, न ही कंप्यूटर से उनका कोई वास्ता है। देश में इस समय लगभग 6 करोड़ लोग ही इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं (देखें मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी की सालाना रिपोर्ट)। तो अगर राजेंद्र यादव या प्रभाष जोशी देश के छह करोड़ कनेक्टेड लोगों में नहीं हैं तो क्या फर्क पड़ता है?
फर्क पड़ता है। इसलिए क्योंकि ये दोनों कम्युनिकेशन यानी संवाद के धंधे में हैं। और ऐसे लोग अगर दीन-दुनिया से अपडेट न रहें तो फर्क पड़ता है। ये बेखबर लोग अगर अपनी बात खुद तक ही रखें तो हमें धेले भर की परवाह नहीं। लेकिन वो बोल रहे हैं और बेहद बेतुका और बेहूदा बोल रहे हैं। ये दोनों लोग ऐसी बातें बोल रहे हैं, जो उनके चेलों के अलावा हर किस को अखर रही है। मैं एक भी ऐसे आदमी को नहीं जानता, जो जातिवाद के समर्थन में उनके विचारों का कम से कम सार्वजनिक तौर पर समर्थन करें। इन दोनों महान लोगों के चेलों के पास भी बचाव में देने को कोई तर्क नहीं हैं। आखिर इनके चेलों में से भी कई ने जाति से बाहर शादी की है। उन्हें मालूम है कि उनकी अगली पीढ़ी क्या करने वाली है। हर जाति के लोगों को ये लेखन आउटडेटेड और सड़ा हुआ लग रहा है। 21वीं सदी के लगभग 10 साल बीतने के बाद ये अज्ञानी लेखन हमारी देवभाषा में ही संभव है। इस समय पश्चिम में आप कल्पना नहीं कर सकते कि कोई जाति या वर्ण या नस्ल या रंग के आधार पर श्रेष्ठता का ऐसा खुल्लमखुल्ला और अश्लील समर्थन करे। उसे पूरा देश दौड़ा लेगा।
बहरहाल ये इस बात का प्रमाण है कि ये दोनों लोग दुनिया में चल रहे आधुनिक विमर्श से वाकिफ ही नहीं हैँ। ये महानगर में रहते हैं। आर्थिक रूप से समर्थ हैं। लेकिन नेट पर नहीं हैं। पता नहीं की-बोर्ड पर काम करना इन्हें आता भी है या नहीं। ऐसे में दोनों को पता ही कैसे चलेगा कि नॉम चॉमस्की ने अपने ब्लॉग पर ताजा क्या लिखा है या फिर फ्रांसिस फुकोयामा के बारे में ब्लॉग में क्या चल रहा है। उन्हें पता ही नहीं कि दुनिया कितनी बदल गयी है। नहीं, ये एलीट होने या जेब में ढेर सारे पैसे होने की बात नहीं है। 10 रुपये में कोई भी आदमी आधे से लेकर एक घंटे तक इंटरनेट कैफे में कनेक्ट हो सकता है। प्रभाष जोशी और राजेंद्र यादव भी ये कर सकते हैं। वो ऐसा नहीं करते, इस वजह से उनका अपने पाठकों की दुनिया से जबर्दस्त डिस्कनेक्ट है।
भारत में इतने हमलावर आये हैं (उनमें से ज्यादातर अपने साथ परिवार लेकर नहीं आये) और समाज व्यवस्था में इतनी उथल-पुथल हुई है कि रक्त शुद्धता की बात कोई कूढ़मगज इंसान ही कर सकता है। हिमालय के किसी बेहद दुर्गम गांव में या किसी द्वीप या किसी बीहड़ जंगल में बसी बस्ती के अलावा रक्त अब शायद ही कहीं शुद्ध बचा होगा। ऐसे में कोई ये कहे कि कोई खास जाति किसी खास काम को करने में इसलिए ज्यादा सक्षम और समर्थ है कि उसका जन्म किसी खास जाति में हुआ है, तो इस पर आप हंसने के अलावा क्या कर सकते हैं। आप रो भी सकते हैं कि जिन लोगों को हिंदी भाषा ने नायक कह कर सिर पर बिठाया है, उनकी मेधा का स्तर ये है।
प्रभाष जोशी और राजेंद्र यादव, क्या आपको अपने घरों में नयी पीढ़ी की हंसी की आवाज़ सुनाई दे रही है? पता लगाइए कि कहीं वो आप पर तो नहीं हंस रहे हैं।
प्रभाष जोशी तो खुद को ब्राह्मण ही मानते होंगे। उनमें वो सारे गुण होंगे, जिनका जिक्र उन्होंने ब्राह्मणों के बारे में अपने इंटरव्यू में किया है। अगर उनका जन्म मिथिलांचल या मालवा के किसी बेहद गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ होता, तो भी क्या ये तय था कि वो संपादक ही बनते। इस बात की काफी संभावना है कि वो पटना या इंदौर के किसी सरकारी दफ्तर में चपरासी होते और लोगों को पानी पिला रहे होते। राजेंद्र यादव किस जातीय गुण की वजह से संपादक बन गये?
तो प्रभाष जोशी और राजेंद्र यादव,
बात सिर्फ इतनी सी है कि किसी को कितना मौका मिला है। बात अवसर की है। ये न होता तो आप अपने बच्चों को किसी गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाते। फिर हम भी देखते धारण क्षमता का चमत्कार। यादव जी का ये कहना गलत है कि “ब्राम्हणों में कुछ चीज़ें से अभ्यास आयी हैं जैसे कि अमूर्तन पर विचार-मनन और इसीलिए कविताई में उनका वर्चस्व है। इन्हीं वजहों से विश्वविद्यालयों और अकादमियों में भी वे काबिज़ हैं।” वो वहां काबिज इसलिए हैं, क्योंकि उन्हें वहां तक पहुंचने का मौका मिला है। पढ़ाई-लिखाई को लेकर चेतना अलग-अलग जातियों और समूहों में कुछ जादू नेटवर्किंग का भी है। नरेंद्र जाधव और बीएल मुणगेकर को मौका मिला तो दलित होते हुए भी वो पुणे और मुंबई जैसे बड़े विश्वविद्यालयों में कुलपति बन गये। कोई भी बन सकता है।
किसी जाति में कोई अलग गुण नहीं होता। कुछ पुरानी बातें अब लागू नहीं होतीं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने गीता का भाष्य करते हुए 18वें अध्याय में यही कहा है। पढ़ लीजिएगा। 21वीं सदी में जातीय श्रेष्ठता की बात करेंगे तो घृणा के नहीं हंसी के पात्र बनेंगे।
ये वक्त के साथ खुद को बदल नहीं पाए!
मेरे करीबी रिश्तेदारों में कई जातियों के लोग हैं। ब्राह्मण से लेकर कायस्थ और नायर से लेकर दलित तक। ये सभी सभी परिवार प्रेम से रह रहे हैं। आपके परिवारों में भी लोगों ने प्रेम किया होगा और कई ने जाति से बाहर शादियां भी की होंगी। अब आप जाति पर अपने शर्मसार करने वाले विचारों को अपने रिश्तेदारों पर लागू करके देखिए और हिसाब लगाइए कि कौन सी बच्ची या बच्चा कवि बनेगा और कौन कहानीकार और और कौन आत्मकथा बेहतर लिखेगा। या हिसाब लगाइए इस बात का कि कौन बैटिंग करेगा और कौन बॉलिंग और कौन टिक कर खेलेगा और कौन टिककर नहीं खेलेगा या फिर कौन बेहतर नेतृत्व क्षमता दिखाएगा और कौन नहीं दिखाएगा। आपको अपने ही विचारों से शायद नफरत होने लगे और आप अपने बच्चों और पोते-पोतियों से माफी मांगने के अलावा कुछ और नहीं कर पाएं। बड़े लोग जब इस तरह अश्लील और समाज में नफरत फैलाने वाली बातें करने लगें तो हमारा सिर शर्म से झुक जाता है।
मैं ये सोचने की कोशिश कर रहा हूं कि ये दोनों बुजुर्ग बीमार क्यों हैं। इसका एक कारण तो मुझे समझ में आ रहा है। इन्हें दुनिया की शायद खबर ही नहीं है। प्रभाष जोशी इंटरनेट नहीं देखते। वो ऑर्कुट पर नहीं हैं। वो फेसबुक में भी नहीं हैं। मुझे नहीं मालूम कि उनके पास ई-मेल आईडी है या नहीं। कुछ समय पहले तक उनके पास मोबाइल फोन भी नहीं था। एसएमएस पता नहीं वो करते हैं या नहीं। वो ट्विटर पर ट्विट भी नहीं करते। उनका कोई ब्लॉग भी नहीं है। राजेंद्र यादव का भी कमोबेस यही हाल है। वैसे तो इस गरीब देश के ज्यादातर लोगों के प्रोफाइल नेटवर्किंग साइट पर नहीं हैं, वो ईमेल भी नहीं करते, न ही कंप्यूटर से उनका कोई वास्ता है। देश में इस समय लगभग 6 करोड़ लोग ही इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं (देखें मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी की सालाना रिपोर्ट)। तो अगर राजेंद्र यादव या प्रभाष जोशी देश के छह करोड़ कनेक्टेड लोगों में नहीं हैं तो क्या फर्क पड़ता है?
फर्क पड़ता है। इसलिए क्योंकि ये दोनों कम्युनिकेशन यानी संवाद के धंधे में हैं। और ऐसे लोग अगर दीन-दुनिया से अपडेट न रहें तो फर्क पड़ता है। ये बेखबर लोग अगर अपनी बात खुद तक ही रखें तो हमें धेले भर की परवाह नहीं। लेकिन वो बोल रहे हैं और बेहद बेतुका और बेहूदा बोल रहे हैं। ये दोनों लोग ऐसी बातें बोल रहे हैं जो उनके चेलों के अलावा हर किस को अखर रही है। मैं एक भी ऐसे आदमी को नहीं जानता जो जातिवाद के समर्थन में उनके विचारों का कम से कम सार्वजनिक तौर पर समर्थन करें। इन दोनों महान लोगों के चेलों के पास भी बचाव में देने को कोई तर्क नहीं हैं। आखिर इनके चेलों में से भी कई ने जाति से बाहर शादी की है। उन्हें मालूम है कि उनकी अगली पीढ़ी क्या करने वाली है। हर जाति के लोगों को ये लेखन आउटडेटेड और सड़ा हुआ लग रहा है। 21वीं सदी के लगभग 10 साल बीतने के बाद ये अज्ञानी लेखन हमारी देवभाषा में ही संभव है। इस समय पश्चिम में आप कल्पना नहीं कर सकते कि कोई जाति या वर्ण या नस्ल या रंग के आधार पर श्रेष्ठता का ऐसा खुल्लमखुल्ला और अश्लील समर्थन करे। उसे पूरा देश दौड़ा लेगा।
बहरहाल ये इस बात का प्रमाण है कि ये दोनों लोग दुनिया में चल रहे आधुनिक विमर्श से वाकिफ ही नहीं हैँ। ये महानगर में रहते है। आर्थिक रूप से समर्थ हैं। लेकिन नेट पर नहीं है। पता नहीं की-बोर्ड पर काम करना इन्हें आता भी है या नहीं। ऐसे में दोनों को पता ही कैसे चलेगा कि नॉम चॉमस्की ने अपने ब्लॉग http://www.zmag.org/blog/noamchomsky पर ताजा क्या लिखा है या फिर फ्रांसिस फुकोयामा के बारे में ब्लॉग में क्या चल रहा है http://en.wordpress.com/tag/francis-fukuyama/। उन्हें पता ही नहीं कि दुनिया कितनी बदल गई है। नहीं, ये एलीट होने या जेब में ढेर सारे पैसे होने की बात नहीं है। 10 रुपए में कोई भी आदमी आधे से लेकर एक घंटे तक इंटरनेट कैफे में कनेक्ट हो सकता है। प्रभाष जोशी और राजेंद्र यादव भी ये कर सकते हैं। वो ऐसा नहीं करते इस वजह से उनका अपने पाठकों की दुनिया से जबर्दस्त डिस्कनेक्ट हैं।
भारत में इतने हमलावर आए हैं (उनमें से ज्यादातर अपने साथ परिवार लेकर नहीं आए) और समाज व्यवस्था में इतनी उथल पुथल हुई है कि रक्त शुद्धता की बात कोई कूढ़मगज इंसान ही कर सकता है। हिमालय के किसी बेहद दुर्गम गांव में या किसी द्वीप या किसी बीहड़ जंगल में बसी बस्ती के अलावा रक्त अब शायद ही कहीं शुद्ध बचा होगा। ऐसे में कोई ये कहे कि कोई खास जाति किसी खास काम को करने में इसलिए ज्यादा सक्षम और समर्थ है कि उसका जन्म किसी खास जाति में हुआ है तो इस पर आप हंसने के अलावा क्या कर सकते हैं। आप रो भी सकते हैं कि जिन लोगों को हिंदी भाषा ने नायक कहकर सिर पर बिठाया है, उनकी मेधा का स्तर ये है।
प्रभाष जोशी और राजेंद्र यादव, क्या आपको अपने घरों में नई पीढ़ी की हंसी की आवाज सुनाई दे रही है। पता लगाइए कि कहीं वो आप पर तो नहीं हंस रहे हैं।
प्रभाष जोशी तो खुद को ब्राह्मण ही मानते होंगे। उनमें वो सारे गुण होंगे जिनका जिक्र उन्होंने ब्राह्मणों के बारे में अपने इंटरव्यू में किया है। अगर उनका जन्म मिथिलांचल या मालवा के किसी बेहद गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ होता तो भी क्या ये तय था कि वो संपादक ही बनते। इस बात की काफी संभावना है कि वो पटना या इंदौर के किसी सरकारी दफ्तर में चपरासी होते और लोगों को पानी पिला रहे होते। राजेंद्र यादव किस जातीय गुण की वजह से संपादक बन गए?
तो प्रभाष जोशी और राजेंद्र यादव,
बात सिर्फ इतनी सी है कि किसी को कितना मौका मिला है। बात अवसर की है। ये न होता तो आप अपने बच्चों को किसी गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाते। फिर हम भी देखते धारण क्षमता का चमत्कार। यादव जी का ये कहना गलत है कि “ब्राम्हणों में कुछ चीज़ें से अभ्यास आई हैं जैसे कि अमूर्तन पर विचार-मनन और इसीलिए कविताई में उनका वर्चस्व है। इन्हीं वजहों से विश्वविद्यालयों और अकादमियों में भी वे काबिज़ हैं। “ वो वहां काबिज इसलिए हैं क्योंकि उन्हें वहां तक पहुंचने का मौका मिला है। पढ़ाई लिखाई को लेकर चेतना अलग अलग जातियों और समूहों में कुछ जादू नेटवर्किंग का भी है। नरेंद्र जाधव और बीएल मुणगेकर को मौका मिला तो दलित होते हुए भी वो पुणे और मुंबई जैसे बड़े विश्वविद्यालयों में कुलपति बन गए। कोई भी बन सकता है।
किसी जाति में कोई अलग गुण नहीं होता। कुछ पुरानी बातें अब लागू नहीं होतीं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन मे गीता का भाष्य करते हुए 18वें अध्याय में यही कहा है। पढ़ लीजिएगा। 21वीं सदी में जातीय श्रेष्ठता की बात करेंगे तो घृणा के नहीं हंसी के पात्र बनेंगे।
Saturday, August 22, 2009
क्रिकेट के मैदान में अधूरा भारत क्यों दिखता है?
विनोद कांबली का टीम से बाहर होना क्या किसी नस्लभेदी या जातिवादी साजिश की वजह से हुआ था? एक टीवी कार्यक्रम में इस ओर संकेत कर विनोद कांबली ने बेहद संवेदनशील मुद्दा छेड़ दिया। लेकिन एक व्यक्ति के टीम में होने या न होने या निकाले जाने से बड़ा एक मुद्दा है, जिसपर बात होनी चाहिए। वो है क्रिकेट के मैदान में पूरे देश की इमेज नजर न आना। आखिर ये शायद अकेला टीम स्पोर्ट है जिसकी भारतीय टीम में नॉर्थ ईस्ट से कोई नहीं होता, कोई आदिवासी नहीं होता, कोई दलित नहीं होता, पिछड़े जाति समूहों के खिलाड़ी आम तौर पर नदारद होते हैं। यानी तीन चौथाई से ज्यादा हिंदुस्तान भारतीय क्रिकेट टीम में नजर ही नहीं आता। और ये साल दर साल से चला आ रहा है।
24 साल की उम्र में विनोद कांबली की टेस्ट क्रिकेट से विदाई से कुछ असहज सवाल तो खड़े होते ही हैं। विनोद कांबली ने 1992-93 में इंग्लैंड के खिलाफ सिरीज से टेस्ट करियर की शुरुआत की और उन्होंने 17 मैचों में 1084 रन बनाए। उन्होंने इस दौरान 4 सेंचुरी और 3 हाफ सेंचुरी बनाई। उनका टॉप स्कोर 227 रहा और बैटिंग एवरेज रहा 54.20 (सचिन तेंडुलकर का एवरेज है 54.58)। आखिर के चंद टेस्ट मैच में कांबली जरूर ढलान पर रहे। लेकिन अगर अजित आगरकर लगातार पांच टेस्ट इनिंग्स मे जीरो बनाकर भी इंडियन टीम में रह सकते हैं और कई खिलाड़ियों (सचिन और गांगुली समेत) की खराब फॉर्म के बाद टीम में वापसी होती रही है तो ये सवाल उठता ही है कि कांबली जैसे टैलेंटेड खिलाड़ी को प्रदर्शन सुधारने का टेस्ट मैच में एक भी मौका क्यों नहीं मिला। तेज शॉर्ट पिच गेंदों को खेलने की उनकी जिस कमजोरी की बात की जाती है वो तो गांगुली समेत देश के कई बैट्समैन के साथ रही है। तकनीक में सुधार का मौका मिलने में कई बैट्समैन ने इस कमजोरी को सुधार भी लिया। ये सुविधा कांबली को नहीं मिली और इसे ही संभवत: वो भेदभाव कह रहे हैं।
बहरहाल विनोद कांबली की टीम से विदाई के बाद ये सवाल एक बार फिर सामने आ गया है कि भारतीय टीम में पूरा भारत क्यों नहीं दिखता। ऑस्ट्रेलिया के एक खेल पत्रकार ने साइमंड्स और हरभजन विवाद के समय भारतीय क्रिकेट में ब्राह्मण वर्चस्व के बारे में पूछा था तो क्रिकेट जगत में जबर्दस्त विवाद खड़ा हो गया था। किसी को ये सवाल जातिवादी, सैक्टेरियन, विभाजनकारी और मॉडर्निटी विरोधी लग सकती है लेकिन ऐसी बहस तो इस समय लगभग पूरी दुनिया में चल रही है और लगभग सभी विकसित देश एक के बाद एक ये मान रहे हैं कि राष्ट्र की विविधता राष्ट्रजीवन के तमाम अंगों में उसी खूबसूरती से नजर आना देश और नागरिकों के हित में है।
ऐसे देशों में अमेरिका (जहां अब एक अश्वेत राष्ट्रपति है), फ्रांस, कैनेडा, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। ये सभी देश डायवर्सिटी को अपना रहे हैं। ब्रिटेन की क्रिकेट टीम में चेन्नई का जन्मा एक मुसलमान नासिर हुसैन कैप्टन बनता है और फ्रांस अपनी फुटबॉल टीम की कमान अफ्रीकी मूल के जिनाडिन जिडान को सौंप सकता है। हॉलैंड की फुटबॉल टीम में लगभग आधा दर्जन अश्वेत नजर आते हैं। एक और मिसाल के तौर पर साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम को ही लीजिए। वहां के क्रिकेट बोर्ड के डायवर्सिटी प्लान के तहत टीम में लगभग आधे खिलाड़ी ब्लैक या मिली जुली नस्ल के होते हैं और इसमें भारत समेत एशियाई मूल के खिलाड़ी भी शामिल हैं।
नहीं ये कोई कोटा सिस्टम नहीं है। अगर वंचित तबकों को आगे लाने का मतलब मेरिट की अनदेखी होता, तो फ्रांस और हॉलैंड की फुटबॉल टीम कमजोर टीमों की गिनती में आती और साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम दुनिया की सबसे कमजोर टीम होती। लेकिन ऐसा नहीं है। अश्वेतों की भागीदारी ने साउथ अफ्रीका की टीम को कमजोर नहीं किया। आईसीसी की वन डे रैंकिंग में फिलहाल वह नंबर वन है। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि 1983 में जिस क्रिकेट टीम में विश्वकप जीता था, उसमें भारतीय समाज की विविधता शायद अब तक सबसे बेहतरीन शक्ल में नजर आई थी। दरअसल खेल में डायवर्सिटी का एक ही मतलब है और वो है टैलेंट पूल को बड़ा करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों तो खेलों को ले जाना। क्रिकेट तो वैसे भी 12 देशों का खेल है। अगर भारत को स्पोर्ट्स सुपरपावर बनना है, ओलिंपिक्स में मेडल लाने हैं तो देश में टैलेंट पूल को कई गुना बढ़ाना होगा।
अब जबकि आईपीएल के रूप में इतना अधिक क्रिकेट खेला जा रहा है और इतने ज्यादा खिलाड़ी मैदान में हैं कि टैलेंट को दबा पाना आज उस तरह संभव नहीं है जैसा कि आज से 20 या 50 साल पहले हो सकता था। आज तो किसी छोटे शहर का धोनी, प्रवीण कुमार, हरभजन सिंह या आरपी सिंह तमाम बाधाओं को पार कर टीम में जगह बना लेता है। साधारण परिवार से आने वाले अमित मिश्रा के टेलेंट की अनदेखी आज मुश्किल है।
इसके बावजूद क्रिकेट में अगर हॉकी या फुटबॉल या एथेलेटिक्स जैसी विविधता वाली टीम नजर नहीं आती तो इसकी वजह क्रिकेट के इतिहास और इस खेल के स्वरूप में है। आजादी से पहले तक क्रिकेट टीम में ज्यादातर राजा-महाराजा हुआ करते थे। उसके बाद भी क्रिकेट जिमखाना संस्कृति से अरसे तक मुक्त नहीं हुआ। साथ ही क्रिकेट का एक और केंद्र वो स्कूल और कॉलेज रहे जहां अच्छे मैदान थे, नेट पर क्रिकेट के गुर सिखाने वाले अच्छे कोच थे और इन स्कूलों में प्रवेश हर किसी को नहीं मिल सकता था। इसलिए क्रिकेट का एक एलीट चरित्र हमेशा से रहा।
क्रिकेट के बारे में कई समाजशास्त्रियों ने ये बात लिखी है कि ये खेल मूल रूप से भारतीय स्वभाव के अनुकूल है। इसमें शारीरिक संपर्क न्यूनतम है और ये छुआछूत मानने वाली भारतीय जाति परंपरा के भी हिसाब से फिट खेल है।
लेकिन वक्त के साथ क्रिकेट भी बदल रहा है। अब ट्वेंटी-ट्वेंटी फॉर्मेट में स्टैमिना का महत्व काफी बढ़ गया है। खेल का चरित्र बदलने के साथ ही खेलने वाले भी बदल रहे हैं। कांबली की शिकायत उनके समय के हिसाब से सही हो भी सकती है लेकिन 2009 के भारतीय क्रिकेट के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। आने वाले दिनों में किसी कांबली को शायद ये शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा कि जाति की वजह से उसे टीम से निकाल दिया गया
Tuesday, August 18, 2009
किसके नाम पर जलाएं उम्मीद के दीये
शुरुआत पूजा प्रसाद की इन पंक्तियों से...
आइये उम्मीद जगाएं
ईश्वर के नाम पर जलाएं कुछ दीये
और इन दीयों से असंख्य देहरी टिमटिमाने की
आस बनाएं...
आइये उम्मीद जगाएं।
कविता आगे बढ़ती है, पूरी कविता आप उनके ब्लॉग पर पढ़ सकते हैं, पर यहाँ मैं आपका ध्यान इस पर आयी अनुराग अन्वेषी की टिप्पणी की तरफ़ खींचना चाहता हूँ :
गुम हुए हजारों नट और सपेरे की तरह ही हो गए हैं आस्था और भरोसा। और अफसोस है कि मिनट भर का करतब दिखाने वाले ईश्वर (वैसे अबतक उसका कोई करतब देखा नहीं हूं, सिर्फ सुनता आया हूं दूसरों के मुंह से) के नाम पर ही दीये जलाए जाते हैं। आइए, आस्था और भरोसे के साथ हम इनसान बने रहने की कसम खाते हुए दिये जलाएं। :-)
अपनी बात मैं अनुराग जी की टिप्पणी से शुरू करना चाहता हूँ। उनका यह अफ़सोस समझ में आता है कि दीये ईश्वर के नाम पर ही जलाये जाते हैं। अफ़सोस ज्यादा गहन इसलिए भी हो जाता है यह पहल पूजा प्रसाद जैसे लोगों की तरफ़ से होती है। उम्मीद के दिए जलाना हर समाज के लिए जरूरी होता है। हर दौर में और हर तरह की परिस्थिति में यह एक जरूरी काम होता है। स्थिति जितनी प्रतिकूल हो उम्मीद के दीये जलाना उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है। यह समाज के लिए संजीवनी का काम करता है, उसे मुर्दा बन जाने से रोकता है।
कहने की जरूरत नही कि ऐसी महत्वपूर्ण भूमिका समाज का वही हिस्सा अपने हाथ में लेता है जो उसका सबसे संवेदनशील, सबसे समझदार और सबसे जिम्मेदार हिस्सा होता है। मौजूदा दौर में पूजा प्रसाद जैसे थोड़े से लोग इस भूमिका में दिख रहे हैं। यह हम सब के लिए सुकून देने वाली बात है कि घनघोर निराशा के इस दौर में भी कुछ लोग उज्जवल भविष्य की तरफ़ हमारा ध्यान खींच कर हमें आगे बढ़ने की ताकत दे रहे हैं। लेकिन यही वह बिन्दु है जहाँ अनुराग जी का अफ़सोस सामने आता है और पूरे औचित्य के साथ आता है। अनुराग अन्वेषी का सवाल यह है कि आख़िर दीये ईश्वर के नाम पर ही क्यो जलाए जाते हैं।
अफ़सोस की वजह यह है कि हमारे समाज का सबसे संवेदनशील, समझदार और जिम्मेदार हिस्सा भी इंसानी समाज को इस लायक नही मानता कि उसके नाम पर, इंसानियत के नाम पर उम्मीद के दीये जलाए। उसे इंसानियत नाकाफी लगती है, भरपूर रौशनी वाले उम्मीद के दीये के लिए उसे एक काल्पनिक ही सही, पर ईश्वर चाहिए। ऐसा ईश्वर जिसे इंसानी समाज का सशर्त नही, पूर्ण समर्पण चाहिए होता है। उसे यानी ईश्वर को इंसान का ऐसा मन -मस्तिष्क चाहिए जो सवाल न करता हो, तर्क न करता हो, संदेह न करता हो। जो बस इस बात को अन्तिम सत्य के रूप में स्वीकार कर चुका हो कि ईश्वर जो करता है (और सब कुछ ईश्वर ही करता है ) वह अच्छा ही करता है।
संदेश साफ़ है यह पूरी दुनिया ईश्वर की है, पत्ता भी खड़क रहा है तो उसकी मर्जी से खड़क रहा है। इसीलिये आपको समझ में आए या न आए वह आपके और हर व्यक्ति के भले के लिए ही हो रहा है। तो अब अगर आप उससे असंतुष्ट हैं तो यह या तो आपकी नासमझी है या फ़िर ईश्वर में आपके भरोसे की कमी। दोनों ही स्थितियों में दोष आपका है।
और अगर आप हद से ज्यादा पीड़ित हैं तो उसकी शरण में जाइए, उससे अपनी प्रार्थना बताइये। अगर आप उसके सच्चे भक्त हैं तो वह कभी आपको निराश नही करेगा। यानी पहली बात तो यह कि जो उसके भक्त हैं उन्ही की सुनवायी होगी। जो उसे चुनौती देते हैं उनकी शिकायत का कोई मतलब ही नही बनता। और इस करुणा सागर के दरबार में पहुँच कर भी अगर आपकी शिकायत सुनने लायक नही मानी गयी तो भी आप सर्वशक्तिमान ईश्वर का कोई दोष साबित नही कर सकते। इसका मतलब सिर्फ़ यह होता है कि आप उसके सच्चे भक्त नही हैं। यानी दोष एक बार फ़िर आपका।
मतलब यह कि इस परम परमेश्वर की व्यवस्था में इंसान के अस्तित्व का मतलब सिर्फ़ इतना है कि जो कुछ हो रहा है उसे ईश्वर का आदेश मान चुपचाप स्वीकार करते जाओ। बस उसके गुण गाओ, उसकी तारीफ में कसीदे पढो, हर बात में उसकी शान देखो। भूल कर भी किसी बात पर सवाल मत करो, न ही संदेह करो। और उसके आदेश की अवज्ञा? ऐसा तो सोचो भी मत।
कमाल तो यह है कि इस व्यवस्था को स्वीकारने वाले भक्तों को भी हम मानसिक और भावनात्मक गुलाम नही मानते बल्कि उन्हें ईश्वर का करीबी और इस नाते शक्तिशाली मानते हैं।
मगर यह मूल तर्क के ख़िलाफ़ नही है। चूंकि इस व्यवस्था में ईश्वर सर्वशक्तिमान है और हर तरह की ताकत का स्रोत वही है इसीलिये ताकतवर उसे ही माना जाएगा जो उसका करीबी होगा। और, स्वाभाविक रूप से करीबी वही होगा जो उसकी व्यवस्था को ज्यों का त्यों स्वीकार करेगा।
सोचने समझने वाले जो लोग यह कहते हैं कि आख़िर ईश्वर या धर्म पर सवाल उठाना क्यो जरूरी है, और यह कि धर्म और ईश्वर से टकराए बगैर या दूसरे शब्दों में भारत की श्रद्धालु जनता की आस्था को चोट पहुंचाए बगैर भी तो काम किया जा सकता है, उनके लिए निवेदन है कि यहाँ सवाल किसी की आस्था को चोट पहुंचाने का नही है, सवाल सिर्फ़ यह है कि हमारा इंसानी समाज कैसा होगा, इंसान कैसा होगा। जैसा इंसान होगा इंसानी समाज भी वैसा ही होगा।
ऊपर कही गयी बातों से हमारी यह मान्यता तो स्पष्ट हो ही जाती है कि ईश्वरीय व्यवस्था को पूर्णतया समर्पित, कमजोर बल्कि मानसिक और भावनात्मक तौर पर गुलाम इंसान ही भाते हैं।
हमारी आपत्ति इसी बात को लेकर है। और इसमे बीच का कोई रास्ता नही हो सकता। इंसान या तो स्वतंत्र रूप से सोचने समझने वाला, बिना झिझक सवाल पूछने वाला, तर्क और तथ्य के आधार पर सही उत्तर तलाशने वाला होगा या फ़िर बिना कोई सवाल किए दूसरों की कही बातों को मान लेने वाला, कुछ ख़ास धर्मग्रंथो में दिए गए उत्तरों पर सोचने का भी जोखिम न उठाते हुए ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेने और ज़िन्दगी भर स्वीकार किए रहने वाला।
बस यही दोनों विकल्प हैं और इन्हीं दो में से कोई एक हमें चुनना है। धर्म और आस्था ने पहले से बता रखा है कि उसे कैसा इंसान चाहिए। तर्क ने भी पहले से बता रखा है कि वह कैसा इंसानी समाज चाहता है। हमें और आपको तय करना है कि हम दो में से कौन सा रास्ता चुनते हैं। अगर हम में से कुछ लोग किसी भी एक रास्ते को छोड़ने का जोखिम नही लेना चाहते तो यह उनकी निजी समस्या है जिसका हल ख़ुद उन्हें ढूँढना होगा। (प्रसंगवश, अनुराग जी की टिप्पणी का यह हिस्सा कि आइये आस्था और भरोसे के साथ हम इंसान बने रहने की कसम खाते हुए दीये जलाएं ज्यादा सतर्कता की मांग करता है। अनुराग जी को जितना मैं समझ पाया हूँ उसमे उनका यह मतलब कतई नही होगा, लेकिन इससे ऐसा आभास होता है कि शायद दोनों रास्तो पर एक साथ चलना सम्भव है।)
Monday, August 3, 2009
प्रेमचंद और प्रेमचंद की परंपरा में आदिवासी कहाँ हैं?

(झारखंड के प्रमुख संस्कृतिकर्मी पंकज का ये लेख ई-मेल से मिला है। कई पुराने मठो और मूर्तियों के विखंडन के इस दौर में पढ़िए पंकज को।)
2009 की 31 जुलाई के एक दिन बाद जब सारे हिंदी साहित्यकार प्रेमचंद जयंती आयोजनों की थकावट दूर कर चुके होंगे, मैं अपना यह सवाल उनके सामने रखना चाहता हूँ कि प्रेमचंद और प्रेमचंद की परंपरा में आदिवासी समाज कहाँ हैंविनम्र निवेदन यह है कि इस सवाल को ‘आरोप’ नहीं माना जाए और न ही मैं असंदिग्ध रूप से भारत के प्रगतिशील साहित्यकारों में सर्वश्रेष्ठ प्रेमचंद को कठघरे में खड़ा करना चाह रहा हूँ। यह सिर्फ आदिवासी विषय पर सक्रिय एक विद्यार्थी की जिज्ञासा है।
वह इसलिए कि प्रेमचंद की रचनाएँ 1903 से 1936 तक के कालखण्ड में फैली हुई हैं और उन्होंने भारत की उत्पीड़ित जनता के शोषण व यथार्थ को 300 से अधिक कहानियों, एक दर्जन उपन्यासों तथा अनगिनत सामाजिक- राजनीतिक लेखों और समाचारों में समर्थ लेखकीय कौशल के साथ उद्घाटित किया है। वे साहित्य, पत्राकारिता और सांस्कृतिक आंदोलन के मोर्चों पर आजीवन युद्धरत रहे। सामंती और औपनिवेशिक गुलामी के विरूद्ध उन्होंने भारतीय प्रायद्वीप के एक बड़े क्षेत्रा की भाषा हिंदी-उर्दू में हमारा नेतृत्व किया और उनकी कालजयी रचनाएँ एवं विचार आज भी हमारा मार्गदर्शन कर रही हैं। परंतु, प्रेमचंद के संपूर्ण लेखन से गुजरने के बाद भी (शायद कुछ छूट भी गया हो) मेरी यह जिज्ञासा शांत नहीं हो पा रही है कि उनके साहित्य से आदिवासी दुनिया अदृश्य क्यों है? कम से कम उनके बहुचर्चित किसी कहानी, उपन्यास, नाटक या आलेख में तो नहीं ही है।
इस प्रेमचंद जयंती के कुछ दिन पहले मैंने अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए कई मित्रों से बातचीत की। अनेक साहित्यकारों, आलोचकों और पाठकों से यह जानने की कोशिश की कि क्या सचमुच में प्रेमचंद के साहित्य में आदिवासी कहीं नहीं हैं? सबका उत्तर यही था ‘नहीं है’। कई लोग तो यह सवाल सुनकर ही बिगड़ उठे। तुम्हारा/आपका यह सवाल संकीर्णतावादी, गैर-वर्गीय, इलाकावादी और विखंडनवादी है। आम जन के इतने महान लेखक जिनकी कलम की रोशनी से आज भी भारतीय साहित्य (विशेषकर हिंदी) और समाज का मार्गदर्शन हो रहा है, उस पर अंगुली उठाना तुम्हारी/आपकी तुच्छता ही बताती है। लेखक, कलाकार, साहित्यकार और संस्कृतिकर्मी को ऐसे संकीर्ण सोच से देखना कहीं से भी उचित नहीं है। कई लोगों ने कहा - प्रेमचंद तो हमेशा बनारस, इलाहाबाद आदि शहरों में ही ज्यादा रहे। शायद उन्हें आदिवासी समाज को देखने का मौका नहीं मिला होगा।
पहले किस्म के जवाब पर मुझे कुछ नहीं कहना है क्योंकि यह सर्वविदित है कि जब भी वंचित समाज और उत्पीड़ित राष्ट्रीयताएँ अपनी सांस्कृतिक अस्मिता और मुक्ति का सवाल उठाती हैं, उनका दमन इसी सोच के साथ किया जाता है। जो दूसरा जवाब है कि प्रेमचंद शहरों में ही रहे इसलिए वे आदिवासियों के बारे में नहीं जान पाए होंगे, उनको एक संवदेनशील सजग लेखक-पत्राकार के रूप में देखते हुए भी और उनके बनारस व इलाहाबाद में रहने पर भी सही नहीं मालूम होता है। औपनिवेशिक शासन के दिनों में समाचार-सूचना लेने-देने के पेशे से प्रतिबद्धता के साथ जुड़ा समाचार-पत्र का कोई संपादक और आंदोलनकारी पत्राकार कैसे आदिवासी विषय से अनभिज्ञ रह सकता है? वह भी 1900 में जब झारखंड के रांची जिला का दक्षिणी हिस्सा एक बड़े आदिवासी विद्रोह ‘उलगुलान’ से अंग्रेजी शासकों की नींद हराम किये हुए था। इतिहास प्रसिद्ध आदिवासी नायक बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ यह उलगुलान कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले उस समय के अंग्रेजी अखबारों की सुर्खियों में था। और यह भी कि 1899 में प्रेमचंद पहली बार आजीविका के लिए लमही से बाहर निकले थे।
18 रुपये प्रतिमाह पर उन्होंने शिक्षक की पहली नौकरी मिर्जापुर जिला के चुनार में की थी। एक मिशन स्कूल में। विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बसा मिर्जापुर और चुनार प्राकृतिक रूप से आदिवासियों का स्वाभाविक इलाका है। वैसे भी, बनारस से लेकर इलाहाबाद तक विंध्याचल के जंगल-पहाड़ों का जो विस्तार है, उसमें अगरिया, भील, कोरवा, गोंड, कोल, चेरो आदि आदिवासी समुदायों का पारंपरिक निवास है। चुनार में प्रेमचंद ज्यादा समय तक नहीं रहे, परंतु बनारस से चुनार तक की यात्रा और चुनार के अल्प प्रवास में क्या उन्होंने आदिवासी समाज के बारे में कुछ भी नहीं देखा-सुना और जाना होगा? चुनार के बाद प्रेमचंद इलाहाबाद के नजदीक प्रतापगढ़ चले आए थे। जहां वे दो साल रहे। इलाहाबाद से प्रतापगढ़ तक का इलाका भी आदिवासी आबादी से विहीन नहीं है। फिर भी देश-दुनिया का साहित्य पढ़ने तथा पत्राकारिता में रहने का बावजूद उनके साहित्य में आदिवासी जीवन से कहीं मुठभेड़ नहीं होती है।
ध्यान देने की बात है कि बीसवीं सदी की शुरुआत में समाज, राजनीति और साहित्य में सक्रिय सभी लोगों ने दलितों, स्त्रियों और अल्पसंख्यकों के हितों की बात तो की, लेकिन किसी ने भी आदिवासियों के बारे में सोचने की जहमत नहीं उठायी। समाज सुधारक, लेखक और राजनीतिज्ञ, किसी ने भी उन लोगों की सुध लेने की आवश्यकता नहीं महसूस की, जिनकी बेदखली, लूट और नरसंहारों पर नये औद्योगिक भारत की नींव रखी जा रही थी। स्वतंत्राता के पहले भी और स्वतंत्राता के बाद भी। कोयला, लोहा, बाॅक्साइट, लकड़ी और अन्य सभी प्राकृतिक संसाधन जहां से आ रहे थे, इन संसाधनों के जो नैसर्गिक स्वामी थे, उनके साथ क्या हो रहा था यह जानने की कोशिश ही नहीं की गई। क्यों हमारी दृष्टि चार वर्णों तक ही संकुचित है। हमें अपनी ही तरह बलशाली दूसरे धर्म-संप्रदाय तो दिखते हैं, लेकिन वह प्रकृति पूजक एवं आदि धर्मानुयायी आदिवासी नहीं दिखता है। जिसकी आवश्यकताएं सबसे न्यूनतम है और जो सर्वाधिक भाषाओं व संस्कृतियों के बीच बिना किसी टकराव या रक्तरंजित साम्राज्यवादी खेल के आनंद से जीता है। चूंकि अपनी संख्या बल और रिहाइश के आधार पर दलित एवं अल्पसंख्यक समुदाय वोट की राजनीति को प्रभावित करते हैं, इसीलिए उनको अनदेखा नहीं किया जा सका। बाबा साहेब अम्बेडकर की उपस्थिति और दमदार दलित आंदोलनों के कारण भी शासक वर्ग को दलितों की बात सुननी पड़ी। यह अलग बात है कि आज तक व्यवहार में उसका क्या हश्र हुआ। पर हम सभी जानते हैं कि फूले, अम्बेडकर, राजा राम मोहन राय और गाँधी जी जैसे समाज सुधारकों और विचारकों ने दलित, अल्पसंख्यक एवं स्त्री मुक्ति के लिए राष्ट्रीय स्तर पर समाज को आंदोलित किया। चाहे जिसकी जैसी भी जातीय-धार्मिक सीमा या राजनीतिक नीयत रही हो। पर सबने इन शोषित-वंचित समुदायों के लिए कुछ न कुछ कहा। कुछ न कुछ किया।
लेकिन आदिवासी समुदायों के बारे में एक लम्बी चुप्पी इतिहास से वर्तमान तक अजगर की तरह पसरा हुआ है। दुर्गम क्षेत्रों में अपने निवास स्थलों और नगरीय जीवन से अलगाव के कारण आदिवासी आज भी दलितों-अल्पसंख्यकों की तुलना में भारतीय राजनीति पर दवाब डालने की स्थिति में नहीं हैं, पर निःसंदेह वे भारतीय विकास की रीढ़ हैं। उनके संसाधनों पर कब्जा करके ही आधुनिक भारत का विकास संभव हो सका है।
सभी लोग यह स्वीकार करते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा खोने और सबसे कम पाने वाला समाज आदिवासियों का ही है। इतिहास में मुक्ति की सबसे ज्यादा लड़ाईयां आदिवासी समुदायों ने ही लड़ी हैं। उन्होंने भारत के किसी भी समुदाय से सबसे ज्यादा त्याग और बलिदान किया है। प्राकृतिक संसाधनों की लूट और दोहन के लिए वे औपनिवेशिक काल में भी मारे जा रहे थे और आज के स्वतंत्रा भारत में भी मारे जा रहे हैं। कोयलकारो, नेतरहाट, कलिंग नगर, सिंगूर, नंदीग्राम और लालगढ़ इक्कीसवीं सदी के सबसे नये आदिवासी मृत्यु क्षेत्र हैं। लेकिन उनकी चर्चा न तो भारत के मुख्यधारा के समाज में है, न इतिहास में है। हिंदी साहित्य में तो है ही नहीं। जो है वह ‘सॉरी’ बोलने लायक जितना भी नहीं है। यह आदिवासी जिज्ञासा प्रेमचंद से ज्यादा उन लोगों से है, जो अपने आपको उनकी परंपरा का वाहक बताते हैं। जो प्रेमचंद के साहित्य में स्त्री, प्रेमचंद के साहित्य में दलित, प्रेमचंद के साहित्य में अल्पसंख्यक, प्रेमचंद के साहित्य में किसान आदि-आदि विषय सामने लाते हैं और उन्हें भारतीय समाज का सबसे प्रमुख प्रतिनिधि साहित्यकार घोषित करते हैं। प्रेमचंद से छूट गया आदिवासी आज भी उनकी परंपरा से क्यों बहिष्कृत है? प्रेमचंद की परंपरा के लोगों को ‘प्रेमचंद के साहित्य में आदिवासी’ भी लिखना चाहिए। आदिवासी भारत को बहिष्कृत कर कोई कैसे संपूर्ण भारतीय समाज का प्रतिनिधि कहला सकता है? अगर प्रेमचंद की परंपरा और आज के भारतीय साहित्य, समाज और राजनीति में आदिवासी समाज के लिए कोई स्थान नहीं है, फिर तो देश भर के आदिवासी इलाके जिन्हें पूरी तरह से माओवादियों या नक्सलियों के नियंत्राण में बताया जा रहा है, जहाँ पिछले तीन सौ वर्षों से आदिवासी अपने अस्तित्व- अधिकार की अंतिम निर्णायक लड़ाई लड़ रहे हैं, वे आपके साहित्य, समाज और राजनीति को क्यों नहीं खारिज कर दें।
--
A. K. Pankaj
Editor, Johar Sahiya
Flat No. 203, MG Tower,
23, East Jail Road, Ranchi-834001, Jharkhand India
Tel.: +919234301671, 9431109429 , TeleFax: 0651-2562565
Email: akpankaj@gmail.com, johar@sahiya.net
http://www.kharia.in
http://www.akhra.co.in
http://www.sahiya.net http://www.rangvarta.com
http://www.johardisum.in
Wednesday, July 29, 2009
Magic of medieval Patriarchy in a democratic state
It was a Sunday evening। Just before going out to the local market I wanted to update myself on day’s happenings. It landed me up in front of the most objective of the news channels, the NDTV. But it came to be a very disappointing experience of the day. The channel was running a program on young voices of newly elected parliament.
Youngistan was the name given to the program and it was an outdoor exercise in the Garden restaurant in Delhi. All the participants were significant in the sense that they not only represented their constituencies but they are carrying forward the legacy of their families. The carefully chosen group was representing all the important regions of the country- Hamidulla Sayeed (Lakshadweep), Jayant Cahudhary (Mathura), Harsimrat Kuar-badal (Punjab) and Kalikesh Singhdeo (Orissa). Hamidulla is the youngest MP of the country. He is the son of PM Sayeed, former Deputy Speaker of LokSabha. Jyant Chaudhary is the son of Ajit Singh and a grandson of Chuadhary Charan Singh, former Prime Minister of India. Harsimrat is the daughter-in-law of Punjab Chief Minister Prakash Singh Badal and the wife of Deputy Chief Minister of Punjab, Mr. Sukhbir Singh बदल
Junior Sayeed was talking of developing Lakshadweep। Jayant was vowing for rising the issue of farmers. Incidentally he does not have any background of farming except for the fact that his father belongs to a landowning dominant caste of western UP. He has studied in London. Harsimrat was talking of fighting against the practice of female foeticide rampant among the middle and upper middle class of Punjab. Kalikesh is the grand son of a former Chief Minister of Orissa and belongs to a famous royal family of Orissa. He was talking of development though his region is one of the most backward regions of the country despite being rich in resources and his forefathers have ruled the area.
I have given these details to make my point about the appropriation of issues to legitimize their position as the leader of the society and the role of media in establishing their their identity as social leaders। Media has seized questioning. Interestingly, all the participants of this program belong to the families who has been ruling the area since the country became independent. If their areas are backward who is responsible for that?
Unfortunately, the reporter did not ask this question lest it would have destroyed the whole exercise of legitimizing them as social leaders। Harsimarat was step ahead of her co-participants. She has chosen a subject that could make other feel that she is modern and secular and different from her Akali counterparts. The exercise is old one and Bhartiya Janata Party stalwart Mr. Atal Bihari Vajpai has done it long ago.
This ‘benevolent’ politics of Indian elites is the most favorite theme for Indian Media। Medieval patriarchy is being revived to garb the real face of Indian politics. Most of the leaders have transferred their legacies to their sons or daughters or to their family members. The list is very big and it starts from the royal Gandhi family and goes down to local MPs and MLAs.
Media is adding to the confusion created by the new patriarchy evolved after nurturing the vested interests during the post-independence Indian politics। The most dangerous of it is the appropriation of issues of masses. These leaders talk of issues related to the poor people but in reality they serve the interest of rich class. They favor SEZ for development and raise issue of impoverishment of rural people. This dichotomy is conveniently ignored by our media.
The story on Nandigram would add to the points I have raised above। The story was run on IBN7. It was done to depict the changes Nandigram has witnessed in the local power equations after the victory of Trinmool Congress. The issue of land was not mentioned even for a single time and the whole story centered on the power equations affecting the local bureaucracy and political workers of CPM and TNC.
Media is now the biggest tool in raising the issue out of its context and creating confusion among the oppressed classes। The fight between two political and social forces became a quarrel between political parties.
Same evening, Big Bachhan was recalling his days on Times Now. I am sure, he can not recall his contributions in derailing Indian cinema to the extent of making it Lawaris. It is to his credit that Indian cinema got a theme where gangsters became heroes and fighting against the system was an individual endeavor not a social effort. The culmination of the entire struggle was in becoming a tyrant yourself to oppress others. The tradition of Phir Subah Hogi or Jagte Raho or for that matter Boot Polish was lost in a cinematic trend inspired by Hollywood movies. His personal association with Amar Singh speaks volumes about him and his political behavior.
(courtesy : 'communism', the monthly magazine)
Sunday, July 19, 2009
उदयप्रकाश विवाद का सबऑल्टर्न पाठ और हिंदी साहित्य में टीआरपी की व्यवस्था
अच्छा होता अगर योगी आदित्यनाथ के हाथों उदयप्रकाश कोई सम्मान न लेते। लेकिन उतना ही अच्छा होता अगर तमाम प्रगतिशील पत्रिकाओं में बीजेपी और कांग्रेसी और वामपंथी सरकारों के विज्ञापन न छपते (क्या ये बताने की जरूरत है कि भारत में सरकारों का चरित्र क्या होता है)। और शायद उससे भी अच्छा होता कि उदयप्रकाश के आदित्यनाथ से सम्मान लेने के खिलाफ गोलबंदी दिखाने वाले साहित्यकारों ने लालगढ़ में आदिवासियों के संहार के खिलाफ या नंदीग्राम और सिंगुर में राजकीय हिंसा के खिलाफ “भी” ऐसा ही एक वक्तव्य जारी किया होता (मैं जानता हूं कि ये बेहद अश्लील और सांप्रदायिक फासीवादी किस्म की अलोकतांत्रिक मांग है)।
उदयप्रकाश के गलत काम की निंदा में सक्रिय होने वाले साहित्यकारों से ये पूछने का कोई औचित्य नहीं है कि उन्होंने अपने निजी जीवन में कितने ताल-तिकड़म किए हैं। इस लिस्ट में अच्छे-बुरे दोनों होंगे। समानता का बिंदु इनमें सिर्फ ये है कि वो एक मुद्दे पर सहमत हैं। वैसे, उदयप्रकाश या किसी की भी आलोचना के लिए आलोचना करने वाले को 24 कैरेट का होना पड़ेगा, इस तर्क से मैं सहमत नहीं हूं। ऐसी शर्त लगा दें कि पापी पर पहला पत्थर वो मारे, जिसने पाप ना किया हो तो फिर किसी बात की या किसी व्यक्ति की आलोचना ही संभव नहीं है। हम आमतौर पर एक दूसरे को कम या ज्यादा मिलावट के साथ ही स्वीकार कर सकते हैं।
ये पूछना भी बेमानी और बेवकूफी है कि उदयप्रकाश के खिलाफ हस्ताक्षर करने वालों में से कितनों ने कितने रिश्तेदारों और चेलों को कहां फिट कराया है, कितने पुरस्कार किनसे लिए और किनको दिलाए हैं। कितने को और क्यों सबसे प्रतिभाशाली करार दिया है और किसे किस तरह खारिज करने की कोशिश की है। पुस्तक समीक्षाओं और लाइब्रेरी में किताबें लगवाने आदि की अंतर्कथा जानने में भी अपनी दिलचस्पी नहीं है। न किसी से ये पूछने का कोई कारण है कि जिन लोगों को उन्होंने साहित्य में आगे बढ़ाया, उनमें से कितने स्वजातीय थे, कितने चेले थे। ये पूछना भी सरासर बेवकूफी है कि पिछले 10-15 साल में सबसे ज्यादा बिकने वाले दलित साहित्य के रचयिता हिंदी के श्रेष्ठ साहित्यकारों की श्रेणी में स्थान कब पाएंगे। ऐसे सारे सवाल बेमानी हैं।
ये अगर बीमारियां हैं तो ये हिंदी साहित्य का स्थायी भाव भी है। उदयप्रकाश प्रकरण से इसका कोई लेना-देना नहीं है। न ही मेरी दिलचस्पी इस गणना में है कि उदयप्रकाश के खिलाफ हस्ताक्षर करने वाले 60 परसेंट ब्राह्मण-कायस्थ हैं (ऐसी गिनती ब्लॉग पर किसी ने करने की कोशिश की है) या 90 परसेंट सवर्ण हैं। ऐसी गिनती उदयप्रकाश के चेले ही करें। हिंदू समाज की सत्ता संरचना अगर उसी रूप में हिंदी साहित्य में नजर आ रही है तो इस पर अचरज करने का कोई कारण नहीं है। इसके पीछे साजिश ढूंढने वालों को हिंदी और हिंदू समाज की रचना में इसके मूल ढूंढने चाहिए। हस्ताक्षर अभियान में महिलाओं की लगभग गैरमौजूदगी के आधार पर जैसे आप ये नहीं कह सकते कि उदयप्रकाश के खिलाफ पुरुष मिलकर साजिश कर रहे हैं वैसे ही ये नहीं कहा जा सकता कि उनके खिलाफ कोई खास जाति वाले षड्यंत्र कर रहे हैं। महिलाएं यहां भी लगभग गैरमौजूद इसलिए हैं क्योंकि हिंदी साहित्य में ही उनकी मौजूदगी कम है।
जैसे कि किसी जाति का होने से कोई जातिवादी नहीं हो जाता, वैसे ही ब्राह्मणवादी यानी वर्णवादी होने के लिए ब्राह्मण होना कतई जरूरी नहीं है। ठाकुर ही क्यों कई मझौली जातियां अपने उग्र जातिवादी तेवर से कई बार ब्राह्मणों के कान काटती हैं। दलितों का नरसंहार करने में मझौली जातियां सवर्ण जातियों से आगे रही हैं। और उदयप्रकाश जिस जाति के हैं वो तो इस खेल में बराबर की टक्कर देनेवाली जाति मानी जाती है। उपनिषद काल से ही हिंदी वर्णव्यवस्था की दो शीर्ष जातियों की लड़ाई चल रही है। बाकी देश में जब आधुनिकता और अंतर्जातीय विवाहों की आंधी में जाति खत्म हो चुकी होगी और इसकी शुरुआत हो चुकी है, तो भी मेरा अपना अंदाजा है (गलत हो तो खुशी होगी) हिंदी साहित्य के फॉसिल्स में वर्णवाद सबसे प्रभावी तत्व के रूप में मौजूद होगा।
बहरहाल मुद्दे की बात सिर्फ इतनी है कि उदयप्रकाश ने हममे से ज्यादातर की नजर में एक ऐसा काम किया जो हमें नागवार गुजरा है। इसलिए शायद हर लोकतांत्रिक व्यक्ति को इस पर एतराज होगा और इस नाते हमारी नाराजगी उन्हें झेलनी चाहिए। उदयप्रकाश को ये संदेह नहीं करना चाहिए कि अनिल यादव ने किसी जातिवादी साजिश के तहत अमर उजाला में छपे गोरखपुर के समारोह की कटिंग कबाड़खाना ब्लॉग में पेस्ट की थी। अनिल यादव किसी साजिश में शामिल हैं, ऐसा प्रमाण किसी ने अब तक पेश नहीं किया है।
लेकिन एक बात मुझे खटक रही है। उदयप्रकाश ने बेहद तेज नजर पाई है। उनके ऑब्जर्वेशंस के कायल लोगों की कमी नहीं है। जब वो आदित्यनाथ के हाथों सम्मानित हो रहे होंगे तो उन्हें अच्छी तरह मालूम होगा कि वो क्या कर रहे हैं। इतने भोले तो वो नहीं हैं कि इसके असर के बारे में उन्हें अंदाजा नहीं रहा होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि साहित्य में जिस ब्राह्मण-अब्राह्मण विभेद की वो चर्चा करते रहे हैं, उसी धुरी पर वो इस समय पूरे हिंदी साहित्य को नचाने की कोशिश कर रहे हैं। आदित्यनाथ के हाथों सम्मानित होते समय उदयप्रकाश के मन में ये बात रही होगी या नहीं ये कहना तो मुश्किल है लेकिन अब विवाद जहां आ पहुंचा है, वो एजेंडा उदयप्रकाश का ही ज्यादा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जाने अनजाने में हम सब उस एजेंडे के पक्ष या विपक्ष में खड़े हो गए हैं जो उदयप्रकाश ने सेट किया है। वरना इससे पहले आखिरी बार इस बात की गणना कब हुई थी कि साहित्यकारों के किसी समूह में जाति विशेष के कितने लोग हैं।
ये विवाद ब्लॉग और नेट पर तो फास्ट फूड की तरह निबट जाएगा। लेकिन हिंदी के मंथर गति से रेंगते कई साहित्यकारों को अब अगले छह महीने या कई साल तक की जुगाली का माल मिल गया है। इस मामले में आखिरी अध्याय लिखा जाना अभी बाकी है।
यहां एक सवाल उठता है कि क्या हिंदी साहित्य को जातिवाद और ऐसे ही तमाम पोंगापंथी विचारों से मुक्त करने का कोई रास्ता है। क्या इसका एक रास्ता ये हो सकता है कि अंग्रेजी या दुनिया की कई और भाषाओं की तरह हिंदी में भी ये बात सार्वजनिक की जाए कि बेस्टसेलर कौन है? कम से कम तिमाही या छमाही आधार पर अगर प्रकाशकों से उनकी सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों की लिस्ट के आधार पर टॉप 20 या टॉप 100 जैसी कोई लिस्ट बनाई जाए तो शायद कई समस्याओं का समाधान हो जाएगा। दुनिया को ये पता चलेगा कि हिंदी में ज्यादा क्या बिक रहा है। पाठकों के लिए किताबें चुनना आसान हो जाएगी। इसके लिए फिक्शन और नॉन फिक्शन की कटेगरी बनाई जा सकती है। रॉयल्टी की चोरी भी इससे रुकेगी क्योंकि कोई भी प्रकाशक सिर्फ रॉयल्टी बचाने के लिए अपनी किताबों को कम बिकने वाली नहीं बताएगा। सिर्फ लाइब्रेरी में चंद सौ किताबें लगवाकर महान बनने वाले कई सेटिंगबाज साहित्यकारों की इस तरह पोल भी खुल जाएगा। प्रकाशकों की संस्था बेस्टसेलर की लिस्ट बनाने का जिम्मा अपने ऊपर ले सकती है। क्या हिंदी साहित्य और साहित्यकारों में है इतना दम?
औरत- एक वजूद!
औरत
धीरे-धीरे उतरती है
मर्द की जिंदगी में
और शुमार हो जाती है
आदत की तरह.
कभी खौलती है
वजूद में/चाय की तरह
कभी बिखरती है/हर कश के साथ
धुयें की मानिंद.
बहती है कभी रंगों में
जिंदगी की सच्चाई बन
दहक-लाल-गर्म.
थरथराती है कभी/सांसों में
इच्छाओं की
ज्वार भाटा बन.
गोया
पत्नी वजूद नहीं
एक वस्तु हो/जिसे गढा हो
भले ही इश्वर ने
पर/इतना लचीलापन भी जरूरी है
कि मर्द ढाल सके
वक्त-बेवक्त/अपनी सुविधा
और कायदे के सांचे में.
Sunday, July 5, 2009
टाइम मशीन में लालगढ़ और एसपी सिंह
यहां हम एक ऐसे न्यूजरूम की कल्पना करते हैं जहां टाइम मशीन में डालकर लालगढ़ के संघर्ष और एसपी सिंह को एक साथ इकट्ठा कर दिया गया हो। इस घटना के पात्र वास्तविक हो सकते हैं, सिर्फ नाम बदल दिए हैं क्योंकि इससे पूरी बात पर कोई फर्क नहीं पड़ता है।
जून 2009 के आखिरी हफ्ते का कोई दिन
स्थान-एक न्यूज चैनल का दफ्तर
"लालगढ़ में पुलिस के खिलाफ सभा कर रहे 10,000 लोगों को कल आतंकवादी किसने लिखा था?" एसपी की संयत लेकिन थोड़ी तीखी आवाज के साथ ही न्यूजरूम में सन्नाटा छा गया। सुबह साढ़े 9 बजे का समय था। कनॉट प्लेस में टीवी चैनल के एक दफ्तर में रात की शिफ्ट वाले जा रहे थे और अगली शिफ्ट वाले आ रहे थे। हर ओर हलचल मची थी। एसपी सिंह 3 दिन शहर से बाहर रहकर लौटे थे। ज्यादातर लोगों को तो पहली बार में समझ में ही नहीं आया कि लालगढ़ में पुलिस से लड़ रहे लोगों को आतंकवादी नहीं तो और क्या लिखा जाएगा। पूरा मीडिया तो लालगढ़ में जो हो रहा है उसे माओवादी आतंकवादी बनाम सुरक्षा बलों के संघर्ष के तौर पर देख रहा है। ऐसे में एसपी आखिर कहना क्या चाहते हैं।
"भाई ऐसा है कि 10,000 लोग अगर आतंकवादी हो गए हैं और 140 गांवों की पूरी जनता आतंकवादी हो गई है तब तो उन्हें गिरफ्तार करना होगा या मारना होगा", एसपी बोले, " आप सब लोग पत्रकार हैं और इस नाते समझदार भी, क्या ये संभव है।"
न्यूजरूम का सन्नाटा और गहरा हो गया क्योंकि बुलेटिन में आतंकवादी शब्द कई बार आया था और ये खबर कई हाथों से गुजरी थी, जिसमें सीनियर लोग भी शामिल थे। न्यूजरूम की सबसे युवा सदस्य सुनयना ने पूछा, "सर, आतंकवादी नहीं तो क्या लिखें? बंदूक तो उनके पास होती है। हमारे पास जो फुटेज आ रहे हैं उनमें आदिवासियों के हाथों में कुल्हाड़ी, लाठी और दो-चार बंदूकें भी दिखती हैं। उन्होंने लैंडमाइन ब्लास्ट भी तो किए हैं।"
"देखिए अगर हथियार होने से कोई आतंकवादी होता है तो देश में सबसे ज्यादा हथियार तो पुलिस और सेना के पास हैं। उनके काम करने का तरीका भी हिंसक ही होता है। आपकी परिभाषा से तो देश में आतंकवादियों का सबसे बड़ा गिरोह सेना और पुलिस हो गई। मेरे ख्याल से लालगढ़ में जो हो रहा है वो एक पॉपुलर आंदोलन हैं, जिसमें कुछ माओवादी भी घुसे हुए हैं। आप हद से हद इन्हें माओवादी या उग्रवादी या अतिवादी कहें। हिंसक तौर तरीके अपनाने वाले भगत सिंह को ब्रिटेन का इतिहास आतंकवादी कहता है और हम क्रांतिकारी कहते हैं। यानी भाषा के ऐसे सवाल इस बात से तय होते हैं कि आप किस पक्ष में खड़े हैं। मेरी राय है कि पत्रकारों में इस लड़ाई में जनता के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। देखिए आप जैसे ही अपना पक्ष तय करेंगे आपकी भाषा और आपके शब्दों का संस्कार तय हो जाएगा, " एसपी की बात अब कुछ लोगों को समझ में आने लगी थी।
लेकिन सुनयना के जेहन में अभी भी कई सवाल आ रहे थे। वो बोली, "सर, ये लोग सरकार को नहीं मानते, पुलिस को इलाके में घुसने नहीं देते, ऐसे लोगों को आतंकवादी और देशद्रोही क्यों नहीं माना जाए।
एसपी अब गहरी सोच में डूब गए। सुनयना को बाकी सीनियर्स समझाने में जूट गए। कई तरह के तर्क वितर्क होते रहे। अचानक एसपी बोले, सुनयना आपकी राय में लालगढ़ में हंगामा कब शुरू हुआ है। सुनयना के साथ ही कई और लोग बोले लगभग 15-20 दिनों से।
एसपी ने कहा, यही तो हमारे पेशे के लोगों की मुश्किल है। सब कुछ इंस्टेंट होता है आप लोगों के लिए। देखिए अगर पश्चिम बंगाल और देश की बड़ी खबरों पर आपकी नजर होगी तो आपको याद होगा कि पिछले साल नवंबर महीने में इसी इलाके में एक माइन ब्लास्ट हुआ था, जिसमें पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य और उस समय के केंद्रीय स्टील मंत्री रामविलास पासवान बाल बाल बचे थे। वो इलाके में एक स्टील प्लांट के निर्माण का उद्घाटन करने जा रहे थे। इस प्लान्ट के लिए बड़े पैमाने पर जमीन का अधिग्रहण होना है और पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम और सिंगुर के अनुभव के बाद कोई भी किसान सरकार को निजी प्रोजेक्ट के लिए सरकारी कीमत पर जमीन बेचने के तैयार नहीं है। खैर आप सबने भी अपने ही चैनल पर खबर चलाई थी ब्लास्ट के बाद बड़े पैमाने पर लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। इस घटना को जाने बगैर आप लालगढ़ के बारे में अगर लिखेंगे या बोलेंगे तो खबर के साथ और साथ ही उस इलाके की जनता के साथ अन्याय करेंगे। लालगढ़ माओवाद का नहीं जमीन अधिग्रहण और विरोध का मुद्दा है।
इस चर्चा के दौरान दिन की शिफ्ट के ज्यादातर लोग ऑफिस पहुंच चुके थे। कॉन्फ्रेंस रूम में न्यूजमीटिंग के लिए लोग जुटने लगे। चाय के साथ खबरें तय करने का सिलसिला शुरू हुआ...
...न्यूजरूम में लालगढ़ और एसपी सिंह
न्यूज मीटिंग में सभी ब्यूरो से आए आइडिया की लिस्ट और एएनआई और दूसरी समाचार एजेंसियों के दिन के एजेंडे की सूची बांट दी गई। चूंकि लालगढ़ से बेहद एक्साइटिंग विजुअल आ रहे थे। इसलिए ये सब समझ रहे थे कि ये खबर ही आज बिकेगी। लेकिन एसपी ने आतंकवाद और उग्रवाद के बीच फर्क को लेकर जिस तरह अपनी बातें रखीं थी, उससे साफ जाहिर था कि लालगढ़ अब वैसे कवर नहीं होगा, जिस तरह से उसे पिछले तीन-चार दिनों से कवर किया जा रहा था।
एसपी ने बांग्ला के एक अखबार में छपी एक फोटो लोगों को दिखाई। "देखिए ये चार फोटो हैं हमारी आज की सबसे बड़ी स्टोरी।" इसके साथ छपी खबर को पढ़ने के लिए उन्होंने अखबार छवि विश्वास की ओर बढ़ाया। छवि ने जो खबर पढ़ी उसके मुताबिक चूंकि सुरक्षा बलों के पास लैंडमाइन डिटेक्टर सिर्फ दो ही हैं, इसलिए वो आदिवासियों को लोहे की छड़े पकड़ा देते हैं और सुरक्षा बलों के आगे आगे चलने को मजबूर करते हैं। उन्हें कहा जाता है कि वो जमीन को बीच बीच में कोंचकर देखते रहें कि कोई बारूदी सुरंग तो नहीं है।
एसपी ने कहा मुझे कोलकाता से किसी ने बताया है कि वहां के लोकल चैनल के पास इसकी फुटेज है। चैनल के संपादक से मेरी बात हो गई है। कोलकाता की रिपोर्टर से कहिए कि वहां से फुटेज ले आए। इस फुटेज पर बांग्ला चैनल का एक्सक्लूसिव जरूर चलाएं। साथ ही एक रिपोर्टर को फुटेज के साथ मानवाधिकार आयोग भेजिए और वहां से रिएक्शन लाइए। बंगाल के मुख्यमंत्री या चीफ या होम सेक्रेटरी जहां भी मिले उन्हें पकड़िए और सवाल के जवाब में जो भी कहें या चुप रहें, उसे दिखाइए। कोई बात न करे तो रिपोर्टर को राइटर्स बिल्डिंग के बाहर खड़ा कीजिए और उसके रिएक्शन लेने के प्रयासों के बारे में पीटीसी करवाइए। मानवाधिकार आयोग और मुख्यमंत्री कार्यालय में अगले एक घंटे में फैक्स भेजकर रिएक्शन मांगिए।
पिछले तीन दिनों से होम मिनिस्ट्री से आ रहे बयानों और बाइट के आधार पर लालगढ़ की रिपोर्टिंग करने वाले रिपोर्टर प्रकाश चंद्रा को समझ में आ रहा था कि अब उसके आराम के दिन गए। एसपी ने प्रकाश की ओर मुड़कर कहा, "मंत्री और सेक्रेटरी तो बहुत बयान दे रहे हैं। इस बारे में उनसे सवाल पूछिए। जो भी वो कहते हैं उसे स्टोरी के हिस्से के तौर पर डालिए। सरकार असहज सवाल पूछने वालों को ही पूछती है। इसलिए जरा डटकर पूछिए। भरोसा रखिए आपका सोर्स खराब नहीं होगा"
एसपी ने एसाइनमेंट हेड नवीन कुमार से पूछा-लालगढ़ कौन कवर कर रहा है। जवाब मिला कोलकाता की रिपोर्टर श्रुति वहां गई है। वो सुरक्षा बलों के साथ लगातार लगी हुई है और हर पल की खबर चैनल को मिल रही है। इस मामले में हमारा चैनल किसी भी चैनल से पीछे नहीं है।
एसपी ने कहा- अगर सभी चैनलों के रिपोर्टर सुरक्षा बलों के साथ लगे हैं और सारी सूचनाएं सुरक्षा बलों से ही मिल रही है तो कोई भी चैनल पीछे कैसे हो सकता है। लेकिन मुश्किल ये है कि कोई भी चैनल आगे भी नहीं हो सकता। वहां हमारे कम से कम तीन रिपोर्टर और कैमरा टीम होनी चाहिए। एक श्रुति को सुरक्षा बलों से साथ रहने दीजिए। पटना से आशीष और दिल्ली से छवि विश्वास को लालगढ़ भेजिए। दोनों को बांग्ला आती है। ये दोनो रिपोर्टर गांववालों के साथ रहकर उनके नजरिए को सामने लाएंगे। इस तरह हम न सिर्फ बैलेंस रिपोर्टिंग कर रहे होंगे बल्कि बाकी चैनलों को जब तक ये बात समझ में आएगी तब तक हम लीड ले चुके होंगे। हमारे पास अलग तरह के फुटेज होंगे अलग तरह की साउंड बाइट होगी।
एसपी सिंह इस पूरी बातचीत के दौरान बांग्ला और कोलकाता से छपने वाले बाकी अखबारों को पढ़ते भी जा रहे थे। उन्होंने कहा- ये जो खबर इस बांग्ला अखबार में छपी है, इसे देखिए। गांव वाले सुरक्षा बलों को खाने पीने का सामान नहीं बेच रहे हैं। सुरक्षा बलों को उनके साथ जबर्दस्ती करनी पड़ रही है। ये स्टोरी बताती है कि लोगों को सुरक्षा बलों को लेकर कितनी नाराजगी है और दिल्ली के अखबारों में जो छप रहा है कि गांव वालों ने सुरक्षा बलों का स्वागत किया, उसकी हकीकत क्या है।
इसके बाद एसपी डेस्क के लोगों की ओर मुड़े और कहा- देखिए लालगढ़ को पूरे कॉन्टेस्ट में देखिए। ये सिर्फ कानून-व्यवस्था का मामला नहीं है। जमीन अधिग्रहण को लेकर देश भर में जो गुस्सा है, उसके हिस्से के तौर पर भी लालगढ़ को देखा जाना चाहिए। आप लोग कोलकाता के अखबारों को जरूर देखें। उससे आपको ज्यादा पक्षों को समझने में आसानी होगी। दिल्ली में बैठकर आपको ये कैसे अंदाजा लग पाएगा कि वहां के ज्यादातर स्कूलों में फौज भरी है। जीवन अस्तव्यस्त है। वहां लगभग युद्ध जैसे हालात हैं। अपने ही देश की सबसे गरीब जनता के विरुद्ध युद्ध। मैं निजी तौर पर हिंसा के खिलाफ हूं। लेकिन हर तरह की हिंसा का। सरकारी हिंसा का समर्थन मैं नहीं कर सकता। किसान की जमीन मनमानी कीमत पर लेकर उसे उद्योगपतियों को जबरन सौंप देना हिंसा है। दुनिया भर में उद्योगपति खुद जमीन खरीदते हैं। जबरन जमीन ले लेने का ये कानून अंग्रेजों के समय बना। लेकिन आजाद भारत की सरकारें इसका इस्तेमाल करती रहती हैं। ये कानून जनता और किसानों के खिलाफ हिंसा है। हिंसा का विरोध करना है तो इस सरकारी हिंसा का भी विरोध करना चाहिए। ये आश्चर्यजनक है कि सरकार की बंदूकें ऐसे मामलों में हमेशा किसानों के खिलाफ ही चलती हैं। यूरोप या अमेरिका जैसे विकसित लोकतंत्र में इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। ये हमारे जैसे अविकसित देशों में ही हो सकता है।
इस बातचीत को बहुत देर से खामोशी से सुन रहा अभिषेक थोड़ा बेचैन दिख रहा था। अभिषेक ने कहा, "लेकिन सर, माओवादियों को सरकार बैन कर चुकी है। बाजार की ताकतें उनके खिलाफ हैं ही। ऐसे में क्या आपको लगता है कि हमारे जैसा मीडिया इस मुद्दे पर जनता के पक्ष में स्टैंड ले सकता है।"
एसपी के माथे पर चिंता की लकीरें नजर आने लगीं। वो चुप रहे। ऐसा लगा कि वो इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहते। वो धीरे से बोले, "अभिषेक दरअसल आप वो सवाल उठा रहे हैं जो मैं अपने आप से अक्सर पूछता हूं। देखिए आप यहां इतने महीनों से काम कर रहे हैं। चैनल के जनता के या कमजोरों के पक्ष में खड़े होने से आपको शायद ही कभी रोका गया होगा। लेकिन ये तो मानना ही पड़ेगा कि जिसने इस चैनल के चलाने के लिए पैसे खर्च किए हैं वो धर्मार्थ चैनल नहीं चला रहा है। उसे अपने निवेश पर मुनाफा चाहिए। हमें उसने काम पर इसलिए रखा है कि हम उसके लिए मुनाफा कमाएं। इसके लिए जरूरी है कि ढेर सारे लोग हमारा चैनल देखें। अगर आप जनपक्षीय होकर भी दर्शक जुटा पा रहे हैं तो शायद ही आपको कभी टोका जाएगा। बिजनेसमैन की पहली और आखिरी प्राथमिकता पैसे कमाना है। इस गणित को हमें समझना होगा। बिजनेस मैन के पैसे से चल रहे चैनल को हम माओवादियों का मुखपत्र या लघुपत्रिका बनाना चाहेंगे तो वो ऐसा नहीं करने देगा। वो इस चैनल को सरकार का भोंपू भी नहीं बनने देगा अगर ऐसा करने पर दर्शक हमें छोड़ जाएं। इस समय की असली चुनौती है कि कैसे जनपक्षीय होते हुए भी पॉपुलर बने रहा जाए। ये काम कठिन है। लेकिन मुमकिन है। गणेश जी को दूध पिलाने वाली घटना को अंधविश्वास के तौर पर दिखाकर भी दर्शक जुटाए जा सकते थे और अंधविश्वास का खंडन करके भी। हमने मोची के औजार को दूध पिलाकर अंधविश्वास का खंडन किया और पॉपुलर भी बने रहे। ये पत्रकारों के सामने मौजूद सबसे बड़ी चुनौती है।
अभिषेक बीच में ही बोल पड़ा, " लेकिन सर, अगर हमारी रिपोर्टिंग ज्यादा ही जनपक्षीय हो गई तो क्या सरकार और देश के सत्ता इसकी इजाजत देगी। एसपी अब और परेशान नजर आ रहे थे। उन्होंने कहा- "मैं जानता हूं कि इसकी इजाजत संस्थागत मीडिया में नहीं है। मैं संस्थानों के अंदर लोकतांत्रिक और जनपक्षीय स्पेस के लिए गुरिल्ला लड़ाई लड़ रहा हूं। लेकिन ये भी सच है कि महीने के आखिर में मिलने वाली तनख्वाह और संस्थान में होने से आने वाला रुतबा और दबदबा भी शायद मुझे प्रिय है। ये मेरे अंदर का अंतर्विरोध है। कभी कभी मन करता है कि सब छोड़कर चल दूं और अपने मन का काम करूं। लेकिन जो कुछ भी हासिल हो रहा है वो मुझे पीछे खींचता है। इसलिए कई बार मैं समझौते करता हूं। कई बार नहीं करता। कई बार जनता के लिए लड़ रहे संगठनों को पैसे देकर अपना अपराधबोध मिटाता हूं। लेकिन आखिरकार मैं इसी व्यवस्था के अंदर का एक पत्रकार हूं। अपना सच और अपनी सीमाएं मैं जानता हूं। अपनी सीमाएं मैं बढ़ाने की कोशिश में लगा रहता हूं। लेकिन एक लिमिट है, जिसे मैं पार नहीं करता। मुझे कृपया आप लोग इस कमजोरी या सीमा के साथ ही स्वीकार करें।
सुबह की चमक अब एसपी के चेहरे से पूरी तरह गायब हो गई थी। वो थके हुए दिख रहे थे। न्यूजरूम में अब अफरातफरी शुरू हो चुकी थी। इस भाषणबाजी के चक्कर में लगभग डेढ़ घंटे "खराब" हो चुके थे।
Friday, June 26, 2009
12 साल बाद क्यों याद करें एसपी को
जैसा कि एसपी यानी सुरेंद्र प्रताप सिंह ने अपने आखिरी बुलेटिन में कहा था कि ...”लेकिन जिंदगी तो चलती रहती है” और बकौल संवेदनशील कहे जाने वाले कवि अशोक वाजपेयी के, “मरने वाले के साथ कोई मर नहीं जाता,” इस निर्मम-निष्ठुर समय में कुछ लोग एसपी को याद करना चाहते हैं।
एक आदमी जो मठ बनाने में यकीन नहीं करता था और अक्सर हमारे जैसे युवा पत्रकारों से कहता था कि जो घर फूंके आपनो, चले हमारे साथ, वैसे एसपी की याद को लोग आखिर अब तक क्यों जिंदा रखने पर तुले हैं। एसपी कोई चेला मंडली नहीं छोड़ गए। कोई जाति या इलाकाई समूह एसपी के साथ जुड़ा नहीं रहा। उनकी रचनाओं का संकलन या संचयन प्रकाशित कराने वाला कोई नहीं है। ये सवाल तो पूछा ही जाएगा कि एसपी की रचनाओं का संग्रह क्यों नहीं छप पाया।
ये सवाल कई और सवालों की ऋंखला को जन्म देता है। ये असहज करने वाली बाते हैं। एसपी के लेख हिंदी और इंग्लिश में खूब छपे। नवभारत टाइम्स छोड़ने से लेकर टेलिग्राफ ज्वाइन करने के बीच उन्होंने मूल रूप से लिखकर जीवन यापन किया। वो इससे पहले और बाद भी लिखते रहे। इंडिया टुडे से लेकर बिजनेस स्टेंडर्ड में उनके कॉलम छपे। उनके सिंडिकेटेड लेख तो देश भर में छपे। सारा लेखन उपलब्ध है। कोई भी प्रकाशक ये सब छापना चाहेगा। लेकिन ये हो नहीं पाया है।
उनसे कमतर संपादकों की रचनाओं के संकलन देखते-देखते आ गए। बिके न बिके अलग बात है। लेकिन एसपी का लेखन अब भी संकलित रूप में सामने नहीं आ पाया है। ये अफसोस की बात है।
एसपी पिछले कुछ दशकों में हिंदी पत्रकारिता के सबसे बड़े हीरो हैं। लोकप्रियता में उनके आसपास कोई नहीं पहुंच पाया है। लेकिन उनकी स्मृति में डाक टिकट नहीं आया। कई और लोगों के डॉक टिकट आ गए। उनकी स्मृति में कोई महत्वपूर्ण पुरस्कार नहीं है। टेक्स्ट बुक्स में उनका यथोचित उल्लेख नहीं है। उनकी रचनों का संकलन नहीं है। पत्रकारिता की अगली पीढ़ी तक ये बात पहुंचाने का कोई जरिया नहीं है कि एक शख्स ने किस तरह हिंदी पत्रकारिता को आधुनिक बनाने के लिए पायोनियरिंग काम किया। हिंदी टीवी पत्रकारिता की तो एक तरह से विधिवत शुरुआत ही एसपी से होती है। लेकिन क्या ये सब स्मृतियों में ही रहेगा या इसका कोई डॉक्यूमेंटेशन भी होगा।
जो समाज अपने नायकों का सम्मान नहीं करता, वो आगे भी नायकों के लिए तरसते रहने को अभिशप्त होता है। क्या हिंदी का समाज अपनी इस नियति से उबर पाएगा। या टांग खिंचाई और मूर्तियों का खंडन ही इसकी नियति है?
इन बातों पर विचार हम करें या न करें, लेकिन एसपी को याद तो कर ही सकते हैं। इसलिए शनिवार को शाम तीन बजे एसपी को याद करने की योजना कुछ लोगों ने बनाई है। स्थान है प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, रायसीना रोड, नई दिल्ली। आप सब आएं तो कुछ बात बने, कुछ बात बढ़े। वरना जिंदगी तो चलती ही रहती है...
Friday, June 12, 2009
दुश्मन और दोस्त
दोस्त मुझे उन दुश्मनों से बचाना चाहते हैं
दुश्मन रात-दिन ताक में हैं
मेरी हर बात पर, मेरी हर चाल पर उनकी निगाह है
मेरी छोटी-छोटी कमजोरियों को भी
दुश्मन ध्यान से देखते, नोट करते हैं
न जाने कब, कौन सी कमजोरी उनके काम आ जाए
मेरा काम तमाम करने में
दोस्त यह देख विचलित होते हैं
दुश्मन की बारीक नज़र और उनके खतरनाक इरादे
मेरे दोस्तों की नज़र से छुपे नही रहते
वे मुझे उन खतरों से बचाना चाहते हैं
दुश्मन हैं अनगिन
चप्पे-चप्पे पर तैनात हैं दुश्मनों के आदमी
घर में, दफ्तर में, आस-पड़ोस में
मैं घिरा हुआ हूँ दुश्मनों के आदमियों से, दुश्मनों से
दोस्त संख्या में बहुत कम हैं
उन्हें मेरी चिंता है
वे इस लडाई को 'जड़' से ख़त्म कर देना चाहते हैं
वे मुझे समझाते हैं, वे मुझे डराते हैं
वे मुझे वैसा ही बना देना चाहते हैं
जैसा दुश्मन मुझे देखना चाहते हैं
दुशमन कोई रियायत देने को तैयार नही
वे मुझे ज़मीन के हजारों फुट नीचे दफना देना चाहते हैं
ताकि मेरे प्रेत भी वापस न आ सकें उन्हें परेशान करने को
दोस्त मुझे बहुत चाहते हैं
वे मुझे मार कर
मेरी लाश को अपने साथ रखना चाहते हैं
एकदम सुरक्षित
हमेशा-हमेशा के लिए
Sunday, June 7, 2009
Slum in a world of millionaires!
(ऑस्कर की जीत ने 'स्लमडॉग' और 'जय हो' इन दोनों शब्दों को ग्लोबल विस्तार दे दिया। इस नयी लोकप्रियता की बदौलत अब ये दोनों शब्द एक नयी दौड़ में शामिल हो गए हैं। वह है अंगरेजी भाषा का दस लाखवां शब्द बनने की। इस दौड़ में ७३ और शब्द शामिल हैं। बहरहाल, इसी बहाने हम 'स्लमडॉग' की दुनिया की एक झलक ले लेते हैं वरिष्ठ पत्रकार अनिल जी की नज़र से जो नागपुर के लोकमत और मुंबई के जनसत्ता के बाद रायपुर और हैदराबाद की परिक्रमा करते हुए अब दिल्ली आ गए हैं. )
I would start with my some reflections on Slum dog Millionaire because I think that even in an age of small screen explosion; the big screen is still much more effective। I think Slum dog Millionaire is a film which carries a strong statement from the forces of globalization and liberalization. The naked capitalism has shed all its pretensions about humanity and has come out in the open in vulgarizing the dehumanized atmosphere a poor is living in. The film clearly spells out that there is no visible hope in the world poor has woven around them. The change comes from the show business of a globalizing economy but this change is also not without condition.
The film has good number statement about the nation state called India। It depicts a ruthless, cruel, dehumanized society which is communally divided with no regard for human rights। It is a monolithic world of gangsters and corrupt officials (here police)। This post-modernist construct does not trace the origin and development of such a society and tries depicting in matter of fact way, as if the victims themselves have created this society. The brother of the central character has been created to extend a simplistic metaphor where a victim becomes oppressor. The film maker is very much alert that the character does not take up a role of liberator. The like a ad film it takes help of human relationship to sale the idea of a ‘static, ‘inhuman’ and hopeless society of a nation state which has overthrown its colonial masters not many years ago.
We can compare the film with classics like ‘Boot Polish’, ‘Jagate Raho’ or ‘Chakra, a film from alternative cinema। The system has been exposed and horrifying experience of a dehumanized world around has also been depicted with all its details but the belief that life is great and humanity should triumph, has not been lost sight of। We come out by learning lesions to make this world more humane. The learning process by which Jamal comes to win the Kaun Banega Krorepati game show is a very cautiously worked out theme in which the entire third world society has been ridiculed and new Macaulay’s children of globalization has born. The alphabets he learns form the cruel world around is not of compassion or love but of a deep seated lust. The film maker is cautious in depicting the very common theme of sacrificing one’s life for the kin that it should not run into a field where the humanity makes a triumph over the villain design to defeat it. Salim dies for the reason that Jamal should not lose the opportunity of becoming a millionaire. His inspiration for sacrifice comes from the thrilling world of modern market where every one has got a chance to become a millionaire.
The ultimate denial of the nation state comes from an altogether different corner. The legend of Mahanayak has been punctured through a well articulated scene where Jamal baths the filth to meet the great star. The depiction finds its climax in which the host of KBK becomes a villain by trying to stop him from winning the game. Here the disbelief generated against the myth of a Mahanayak is not to create a space for brave and humane kind of heroism. It is a part of grand design of denying the struggle for a democratic and plural society in third world. The agenda is clear a new kind of American Hope should capture our mind. We must refer Noam Chomsky for his depiction of western media. The entire agenda is of manufacturing the Consent. The dog of this slum has not been attributed with the ferocity of the dog Faiz Ahmad Faiz has described,
'ये मजलूम मखलूक गर सर उठायें / तो इन्सान सब सरकशी भूल जाए / ये चाहें तो दुनिया को अपना बना लें/ ये आकाओं की हड्डियाँ तक चबा लें / कोई इनको अह्सासे जिल्लत दिला दे/ कोई इनकी सोयी हुई दुम हिला दे


